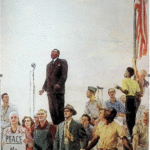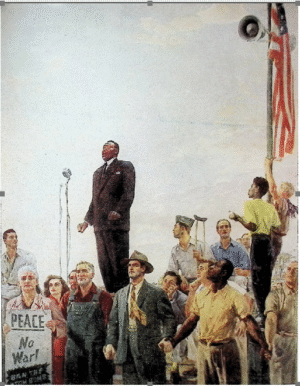भूमिहीनों, गरीबों को उजाड़ना बंद करो; भूमि पर उनका दावा बहाल करो!
(बिहार में जारी वर्तमान भूमि सर्वेक्षण पर जन अभियान, बिहार द्वारा गांधी संग्रहालय, पटना में 9 जनवरी 2025 को आयोजित कन्वेंशन में पेश प्रपत्र।)
जन अभियान, बिहार
बिहार में चल रहे (बढ़ी हुई समय अवधि के साथ) भूमि सर्वे में अफरातफरी की स्थिति दिखती है और यह लोगों की चिन्ता का विषय बना हुआ है। ज्ञात हो कि बिहार सरकार ने 2011 में ही बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम बनाया था। तब भी हम पाते हैं कि अभी तक तैयारी पूरी नहीं है। इस सर्वे में चल रही अफसरशाही, जरूरी कागज़ात के अभाव व धांधली तथा भ्रष्टाचार से ग्रामीण जनता त्रस्त है। और भूमि सर्वे में भूमिहीन होने का तो मतलब ही अलग है! एक बड़ी त्रासदी जो उनके सामने मुंह बाये खड़ी है। वे गांवों में आखिर किसी जमीन के टुकड़े पर बसे हुए तो हैं फिर भी कागजात के अभाव में उनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। पीढ़ियों से गैर-मजरूआ जमीन पर बसे लोग पट्टे के अभाव में कब उजाड़ दिये जायेंगे यह आशंका बनती है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर-बार की जमीन पर किसी और प्रभावशाली रैयत के मालिकाने का हक घोषित कर दिया जाये। समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले ये मजदूर-गरीब किसान जो जातिगत ढांचे के हिसाब से ज्यादातर दलित या अति पिछड़ी जातियों से आते हैं, अपने अनुभव से समाज की इस गति को बखूबी समझते हैं। इनके दावे के हिसाब से सरकार वादे तो करती है लेकिन वे या तो जमीन पर उतरते नहीं हैं या उनको जमीन पर उतारने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। वाजिब व कानूनी हक लेने के लिये भी हर तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। राज्य संघर्ष करने वाले हकदार को या तो कानूनी मामले का वादी बना देता है या फिर अपराधी घोषित कर जेल तक में बंद कर देता है। ऐसी ही राज्य व्यवस्था आज आश्वासन दे रही है कि जिनके पास कागजात नहीं है उन्हें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, सरकार ने उपाय कर दिये हैं। यह आश्वासन भी भूमिहीनों के लिये शायद ही है। चल रहा भूमि सर्वेक्षण इस तबके के लिये अनिश्चितता बन कर आया है। आखिर जो सरकार भूमिहीनों को पहले 3 और फिर 5 डेसिमल बासगीत जमीन देने की बात करती रही है लेकिन पूरा नहीं कर पायी, उसकी बात का क्या भरोसा! इसीलिए मजदूरों-मेहनतकशों के लिए लड़ने वाले संगठनों का यह मंच, जन अभियान, बिहार इस बात को तल्खी से लेता है और सरकार से कहता है कि भूमि सर्वे में भूमिहीन या गैर-मजरूआ व सीलिंग से फाजिल जमीन पर बसे लोगों के मालिकाना हक को कबूल किया जाये। बात तो यहां तक चर्चा में है कि कई जगह भूदान में मिली जमीन को किसानों से वापस लेकर उसके ‘मूल’ मालिकों को वापस किया जा सकता है। गरीबों का इस मामले में बहुत कटु अनुभव रहा है। एक तो जैसा कि हमने बताया हक जताने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, दूसरा, हाल के दिनों में जल, जीवन, हरियाली के नाम पर गरीबों को उजाड़ा गया है। ऐसे में सरकार पर भरोसा करना बेमानी ही लगता है। खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट तक ने भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के उजाड़े जाने को वैध ठहराया है और पर्यावरण के नाम पर गांव की साझी सम्पदा (कॉमन्स) पर से अतिक्रमण हटाने को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के पास हरियाणा में खोरी गांव को कैसे ढाह दिया गया उसका उदाहरण हमारे सामने है। इतिहास के चक्र को घुमाने की ऐसी मुहिम चल रही है कि बेतिया एस्टेट में बसे लोगों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर उजाड़ने की बात हो रही है, हालांकि बसे हुए लोगों को सरकार कुछ राहत देने की बात भी कर रही है। आम तौर पर इस तरह की मुहिमों में धांधली होती है या उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता। ज्ञात हो कि बेतिया एस्टेट का प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत है। बिहार सरकार ने इस एस्टेट की जमीन को अपने मालिकाने में ले लेने का फैसला किया है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरकार उसमें फिर से बंदोबस्ती करने वाली है जिससे हजारों बसे हुए गरीब लोग व किसान प्रभावित होंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जमीन के मामले में राज्य अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुनःबंदोबस्ती या उजाड़ने का काम करने में तत्परता दिखाने लगी है। यहां तक कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सरकारी अनुमोदन व अनुदान से बने घर भी छोड़े नहीं जा रहे हैं। यह भी खटकता है कि जो कोर्ट व सरकारें गरीबों के गांवों तक को उजाड़ने में सोचते तक नहीं वे अतिक्रमण करने वाले अमीरों और रियल एस्टेट बिजनेस की ओर से आंखें मूंद लेते हैं। हम पाते हैं कि पर्यावरण के तमाम नियमों को कमजोर किये जाने और उनका उल्लंघन किये जाने पर कोर्ट चुप रह जाता है परंतु वह पर्यावरण के नाम पर गरीबों द्वारा किये गये तथाकथित अतिक्रमण हटाने पर जोर देता है। भुक्तभोगी ग्रामीण गरीब इसके साक्षी हैं। बांधों के निर्माण में होने वाले विस्थापन से लेकर खनन परियोजनाओं के लिये कॉरपोरेटों द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण का बुरा अनुभव तो हमारे पास है ही।
आखिर इतनी बड़ी मुहिम को आनन-फानन में लेने के पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है? इतनी बड़ी कवायद जो पिछले 50 वर्षों से या उससे भी अधिक समय से नहीं हुई थी या हुई भी तो अधूरी रह गयी उसे क्यों फिर से हाथ में लिया गया? हम समझ सकते हैं कि जो काम कम आबादी की स्थिति में, कम बंटवारे की स्थिति में भी सफल नहीं हुआ उसे यह सरकार तब हाथ में ले रही है जब सरकारी मशीनरी को नव-उदारवादी नीतियों के चलते तनुकृत किया गया है, जिसके चलते आज अल्पकालिक अनुबंध नौकरियों की भरमार है और प्रशिक्षित लोगों की कमी है। प्रशिक्षण को भी आउटसोर्स कर दिया जाता है और यह कम दिनों का ही होता है। सर्वे में मानदेय पर रखे गये अल्पकालिक सेवा के लिए कर्मचारियों को लगाकर कहां तक बेड़ा पार हो सकता है वह सोचनीय है। उनका प्रशिक्षण भी छोटी अवधि का हो रहा है और आनन-फानन में किया जा रहा है। यदि हम व्यवस्थागत भ्रष्टाचार की बात छोड़ भी दें तो अपने इस सर्वे के लिए बने लचर ढांचे में ही अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। जो सरकार नौकरी की परीक्षायें लेने में असफल हो रही है और तमाम अकुशलता व धांधली से पीड़ित है वह इस पूरे सिलसिले में क्या बेहतर काम करेगी? ऐसे में फिर सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? वह कौन सी बात है जो मुम्बई तथा एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी-झोपड़ी धारावी में पीढ़ियों से बसे पट्टाविहीन वाशिंदों को विस्थापित कर उस इलाके के पुनर्विकास के नाम पर बनी योजना के तार को बिहार के जमीन सर्वे से जोड़ती है? याद रहे कि धारावी झुग्गी-झोपड़ी के पुनर्विकास का काम अदानी कॉरपोरेट घराने को दिया गया है जो बेशुमार मुनाफा का स्रोत बनेगा।
जमीन का सर्वे किसी खास मकसद से ही होता रहा है। भले यह लगे कि रैयतों के अधिकारों को यह निबंधित करता है लेकिन यह बात सरकारों के असली मकसद को नहीं दर्शाती है। यह भले सर्वे का सहउत्पाद हो सकता है और किसी भी समय के उत्पादन संबंधों को मालिकाना संबंधों के रूप में मान्यता देकर उस हद तक मालिकों को या रैयतों को भरोसा दिलाता है। तो फिर राज्य की असली मंशा क्या रही है? ब्रिटिश शासन में राजस्व का बड़ा भाग लगान से आता था और इस उद्देश्य से सर्वे करवाये गये (शुरुआती दौर में हमले द्वारा जमीन का औपनिवेशिक हस्तगतकरण भी एक कारण था)। इस व्यवस्था की अहमियत हम इस बात से समझ सकते हैं कि जिला का मुख्य पदाधिकारी कलक्टर कहलाया और उसका मुख्य काम राजस्व वसूली हेतु प्रशासन सम्भालना रहता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने शासन की बागडोर सम्भालते हुए बिहार सहित इस इलाके में स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) की व्यवस्था की थी। जमींदारों को जमीन पर हक दिया गया और उन्हें लगान वसूल कर कम्पनी को और बाद में ब्रिटिश राज को देना पड़ता था। यह एक निश्चित रकम हुआ करती थी। जमींदार तो यह निश्चित रकम देते थे लेकिन उनके लिए फायदेमंद तो यह था कि राज को दिये जाने वाले राजस्व से भी ज्यादा उन्हें मिले। इसके लिए वे जायदाद के रिकॉर्ड बनाने की मुहिम लेते थे ताकि लगान को अधिकतम किया जा सके। ये जमीन के रिकॉर्ड जमीन का रकबा और उसके धारक रैयत का विवरण रखते थे। ये रिकॉर्ड आज भी प्रयोग में लाये जाते हैं और इन रिकॉर्डों में मिलने वाली त्रुटियां आज भी उलझाव का कारण बनती हैं। इसके पहले कि हम इनकी त्रुटियों पर बात करें हम फिर ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जमीन का सर्वे अधिकारों के निबंधन मात्र के लिए नहीं होता बल्कि राज्य व शासक वर्गों के हितों की सेवा करने के लिए होता है। इन हितों की बात हम आगे करेंगे।
बहरहाल हम इस बात पर आयें कि जमींदारी रिकॉर्ड काफी त्रुटियां छोड़ गये। एक त्रुटि जो आज भी विद्यमान है और जिसकी प्रसंगवश चर्चा कर लेनी चाहिए वह है जमीन के डीड का कैथी लिपि में होना जिसे पढ़ना आसान नहीं होता। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड किस हद तक जमींदारी व्यवस्था की विरासत को ढो रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन कानून के लागू होने के बाद ये रिकॉर्ड राज्य सरकार के जिम्मे आ गये और राज्य सरकारें इन्हीं में तब्दिलियां कर काम चलाने लगीं। भूमि सर्वे के विभिन्न रूप होते हैं जिनकी जमीन और उसके मालिक-बटाईदार को चिन्हित करने में अहम भूमिका होती है (cadastral survey, topographical survey, land title survey etc.)। निश्चित रूप से नियमित सर्वे का अभाव जमीन पर वास्तविक हितधारकों के लिए समस्या पैदा करता है। आखिर जमींदारी उन्मूलन के बाद जमीन का पुनर्वितरण हुआ, फिर काश्तकारी (tenancy) सुधार हुए और हदबंदी कानून बना। ये कानून बड़े पूंजीपति-जमींदार राज्य के द्वारा बनाये व क्रियान्वित किये गये थे। बेशक यह इस तरह से किया गया कि उनके वर्ग हितों पर चोट न हो। वास्तव में ऐसी त्रुटियों ने जमींदारों को नये सिरे से बंदोबस्ती कर लेने और रैयतों को बेदखल करने में मदद की। इसीलिए हमारी नज़र में इनको लागू करने के लिए यह भी जरूरी था कि जमीन का सर्वेक्षण होता जो कि नहीं हुआ और खराब रखरखाव वाले तथा त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड ही इस्तेमाल में रह गये। ऐसे में उलझन आते रहे हैं और जमीन विवाद का विषय बना हुआ है। अध्ययन बताते हैं कि ज्यादातर कोर्ट केस जमीन विवाद के ही होते हैं जो लम्बे समय तक लम्बित रहते हैं। ज्ञात हो कि सरकार इस बात से नहीं चिंतित है कि इस तरह रैयतों के खास तबकों की हकमारी होती है या इस सर्वेक्षण से हक मिलने पर मामला सुलझेगा। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है तो सरकार की मंशा में ऐसी सदिच्छा खोजना गलत होगा हालांकि सरकार के पैरोकार लेखक इस तरह की बातें करते हैं।
खराब रखरखाव, कई अलग-अलग विभागों में जमीन रिकॉर्डों का बिखरा होना और आपस में तालमेल न होना, जमीन के मालिकाने हक का अद्यतनीकरण (updating) न होना सरकार के लिए चिंता के विषय इसलिए बने कि इनके चलते जमीन बाजार (land market) अकुशल (inefficient) और बोझिल बना हुआ है। पूंजी निवेश के लिए इस बाजार के विकास और परिपक्वता का होना आवश्यक समझा जाता है। आज रियल एस्टेट का क्षेत्र अग्रणी क्षेत्रों में से है और सरकार इसे तमाम तरीके से बड़ी पूंजी के हक में बढ़ावा देना चाहती है। सरकार चाहती है बाजार में लेनदेन (transactions) त्वरित हों और इस तरह यह बाजार ‘गहरा’ हो। सहज ही समझा जा सकता है कि सरकार की यह मंशा रियल एस्टेट बिज़नेस के फूलने-फलने से जुड़ा हुआ है। यह उन बदलावों को भी दिखाता है जो हमारे सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में आये हैं और इन बदलावों ने जमीन को एक मूल्यवान परिसम्पत्ति (asset) के रूप में ढाल दिया है। पुराने ढर्रे की गृहस्थी करने की प्रवृत्ति लगातार कमजोर होती जा रही है। यह किसान परिवारों की अगली पीढ़ियों की कृषि से निकलने की (मजबूर) अभिलाषा में अभिव्यक्ति पाती है। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र सीएसई के सर्वेक्षण (2012) के अनुसार 67.6 प्रतिशत किसान परिवारों के युवा खेती से निकलना चाहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जिन गांवों तक शहरों का विस्तार होने वाला होता है या हाईवे-एक्सप्रेसवे की जद में जिन गांवों की जमीन आती है वहां के किसान हर्षान्वित होते हैं कि उनकी जमीन के दाम कई गुना बढ़ जानेवाले हैं। इस बार के सर्वेक्षण और 1947 के बाद हुए सर्वेक्षण से उभरी चिन्तायें भी अलग-अलग हैं। बिहार के कुछ जिलों में हुए 1952 से चले सर्वेक्षण ने भाई-भाई में बंटवारे को त्वरित किया और इस तरह निजी हितों को गहरा किया। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ‘परती परिकथा’ में हमें पूर्णिया जिले में चल रहे इस सर्वे का चित्रण मिलता है। आज का सर्वेक्षण एकल परिवारों (nuclear families) के बन जाने की स्थिति में हो रहा है, जहां बंटवारा तो हो गया है लेकिन वह निबंधित नहीं है। इसीलिए वंशावली से लेकर बंटवारे को औपचारिक करने का झंझट रह गया है और ऐसे परिवारों में कागजात की खोज हो रही है। आज सरकारी महकमे की करतूतों से लोग ज्यादा परेशान हैं और दफ्तरों का चक्कर काटने के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। आज के सर्वेक्षण से लोग आपसी कलह से ज्यादा सरकारी मशीनरी के कारनामों से परेशान हैं। इस तरह हो रहे सर्वेक्षण को हमें सामाजिक-आर्थिक बदलावों के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। बिहार सरकार की वेबसाईट भी कहती है कि ”भूमि रिकॉर्ड समकालीन सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और सामाजिक संरचना में हो रहे परिवर्तनों को दर्ज करने के लिए इनका संशोधन और अद्यतनीकरण आवश्यक हो जाता है”।
इन बदलावों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने सर्वे के काम को हाथ में लिया है। जैसा कि हमने कहा ‘लैण्ड मार्केट’ बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में सर्वे पर जोर है ताकि ‘त्रुटियां’ हटायी जा सकें और इस बाजार में सहूलियत से काम किया जा सके। हम त्रुटियों की बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां जिस तरह से मालिकाना हक के इजहार का चलन है वह लेनदेन संबंधी (transactional) और इस तरह अनुमानित (presumptive) किस्म का भी है। खरीदार और विक्रेता के बीच सम्पत्ति के हस्तांतरण में बिक्री की डीड ही मान्य होती है जिसकी रजिस्ट्री करनी पड़ती है। यह रजिस्ट्री उस लेनदेन की होती है। यह जमीन के टाइटल डीड की रजिस्ट्री नहीं होती। अतः इसके आधार पर मालिकाना की गारंटी नहीं हो सकती है और इसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। आज के दिन में भी यह रजिस्ट्री पंजीयन अधिनियम, 1908 के तहत होता है। इसके तहत संपत्ति की बिक्री को पंजीकृत किया जाता है। इसमें केवल खरीदार और विक्रेता की पहचान की जांच होती है। पहचान को सत्यापित करने वाले विभिन्न दस्तावेजों व खास व्यक्ति (जिसे बोलचाल में पहचान कहा जाता है) के द्वारा ऐसा किया जाता है। बेची जा रही भूमि के वास्तविक अवस्थान और उसकी विशेषताओं की जांच निबंधन करने वाला अधिकारी भौतिक रूप से बहुधा नहीं भी करता है। यहां इस बात को भी कह देना जरूरी है कि आजकल निबंधन कार्यालय के कर्मचारी द्वारा जमीन और उसके विक्रेता/क्रेता के फोटो लेने का काम भी होने लगा है। पर इस कार्यालय का काम भी किस बेतरतीब ढंग से होता है उसे कहने की जरूरत नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में वास्तविक मिल्कियत की जांच नहीं हो पाती है। और इसकी वैधता की जांच करने की जिम्मेदारी खरीदने वाले पर है। सरकार इसका सत्यापन नहीं करती। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड और भूमि स्वामित्व की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर हो सकता है। भूमि रिकॉर्डों में त्रुटियां इस स्थिति में उभर कर आ सकती हैं और इस पूरे लेनदेन को चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में उस भूमि पर हो रहे काम या चल रही परियोजना बाधित हो सकती है। सरकार इसी से चिन्तित है।
फिर 1908 के इस कानून के तहत हर लेनदेन में संपत्ति का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। उत्तराधिकार विभाजन के मामले में ऐसा ही है, जिससे मिल्कियत की वैधता संदिग्ध हो सकती है और यह पट्टीदारों के बीच मुकदमों का कारण बनता है। सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण या एक साल से कम के लिए पट्टे पर दी गई जमीन का निबंधन होना भी जरूरी नहीं है।
यह एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। इस सिलसिले में कम्प्यूटरीकरण पर ध्यान दिया गया और इसे आगे बढ़ाया गया जिसका सूत्रपात 1988-89 में ही हो गया था। 2008 में इसे National Land Records Modernization Programme (NLRMP) नामक केन्द्र पोषित स्कीम में बदलकर त्वरित करने की प्रक्रिया चली। इस स्कीम को 2016 में मोदी सरकार ने नाम बदलकर Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) रखा। अब यह केन्द्र सरकार के अंतर्गत है। बिहार में बना ऊपर वर्णित 2011 का सर्वे कानून अपनी प्रस्तावना (vii) में इस बात को रखता है कि ”चूंकि, भारत सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व तथा प्रायोजित भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण में समरूप दृष्टिकोण का अनुपालन नहीं किया गया” (इसलिए सर्वे करना जरूरी है)। हमें इस प्रक्रिया में निहित केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। आखिर जमीन राज्यों के अधिकार क्षेत्र की चीज़ है। जिस तरह रद्द तीन कृषि कानूनों द्वारा इसे उच्छेदित करने का प्रयास हुआ था वह हमारी नजर में है।
हम पाते हैं कि पूरी प्रक्रिया में और सर्वे के हेतु में कीवर्ड (keyword) है ‘निर्णयात्मक स्वामित्व’ (conclusive titling)। जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि यह लैण्ड मार्केट को ‘उन्मुक्त’ ढंग से काम करने देने के लिए है। कम्प्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्डों से आगे इस स्तर पर पहुंचने के लिए सर्वे का महत्व है। यह कहीं से भी भूमिधारकों या किसानों की सहूलियत से प्रेरित नहीं है, हालांकि सहउत्पाद के रूप में यह भूमि के मसले को सुगम करने का काम जरूर कर सकता है। यह बात कि लैण्ड मार्केट से यह प्रक्रिया प्रेरित है और यह व्यवसाय के लिए (खासकर कॉरपोरेट घरानों के लिए) जरूरी है, इसका इस बात से भी पता चलता है कि व्यवसाय करने की आसानी (Ease of doing business) पर बनी संसदीय कमिटी का यह कहना था कि भूमि रिकॉर्डों में गड़बड़ियां लैण्ड मार्केट के ठीक से काम करने में बाधा हैं और इससे विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा पड़ती है। कमिटी ने अनुशंसा की कि जमीन संबंधी सभी रिकॉर्डों को एक जगह सम्मिलित कर एक डेटाबेस बनाया जाये। इसके साथ एक ‘सम्पत्ति पहचान कोड’ का निर्माण हो जिससे किसी भी खास सम्पत्ति के बारे में आसानी से पता लगाया जा सके। यह सब सम्पत्ति के लेनदेन को सुगम और सुनिश्चित बनाने के लिए है ताकि व्यवसाय सम्पत्ति संबंधी बेजा विवादों में न फंसे। हम समझ सकते हैं कि भूमि रिकॉर्डों को कम्प्युटरीकृत कर अगले कदम के रूप में ‘निर्णयात्मक स्वामित्व’ बिज़नेस को सुगम बनाने के लिए जरूरी है। हम पाते हैं कि यह सर्वे किसी भी तरह से किसी प्रगतिशील भूमि सुधार का आगाज नहीं करता। यदि रैडिकल व प्रगतिशील भूमि सुधार के लक्ष्य से इस सर्वे का काम लिया गया होता तो यह सर्वथा स्वागतयोग्य रहता। हां, यह उल्टे कमजोर लोगों को सरकारी (गैर-मजरूआ) जमीन से हटाकर जमीन के एक बड़े रकबे को सरकार को और कालक्रम में कॉरपोरेट घरानों को हस्तांतरित कर सकता है जिसे आगे की अधिरचना परियोजनाओं या अन्य व्यवसायिक काम के लिए काम में लाया जा सकता है। सरकार के लैण्ड पूलिंग और लैण्ड बैंक बनाने की योजना के अंतर्गत ही यह आयेगा। इस पूरी कवायद में गरीब भूमिहीन के कमजोर पलड़े को हम इस विडम्बनापूर्ण स्थिति से देख सकते हैं कि हमें जो विरासत में भूमि रिकॉर्ड मिले हैं वे इस बात को बताते हैं कि जमीन किसके कब्जे में है न कि कौन मालिक है। कब्जा महत्वपूर्ण बात है। इस कब्जे के निर्धारण में उस जमीन के लेनदेन के रिकॉर्ड भी काम आते हैं। पर गरीब लोग जिस जमीन पर काबिज हैं वह मानो मायने ही नहीं रखता। हाशिये पर ठेले हुए इन लोगों पर दखल-कब्जा (possession) का यह फॉर्मूला लागू नहीं होता! सर्वे के वर्ग अंतर्य को समझना चाहिए।
हमने देखा कि भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ करने का अंतिम मकसद ‘निर्णयात्मक स्वामित्व’ की व्यवस्था को स्थापित करना है। बिहार का अधिनियम ‘विकास’ के नाम पर इसे प्रस्तावना (x) में जगह देता है – ”चूंकि, भूमि विकासात्मक गतिविधियों का मूलाधार है; वर्तमान स्वामित्व, दखल एवं भूमि के वर्गीकरण को अंतिम रूप से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ताकि भू-अर्जन का प्रचालन निराधार दावों, कपट एवं जालसाजी से दूषित न हो और साथ ही कृषि ऋण, अनुदान, सहायता तथा बीमा से संबंधित गतिविधियां सुगमतापूर्वक चलाई जा सकें।” यह देशी-विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हितों से प्रेरित व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए किया जायेगा। वित्त पूंजी भी इस ओर बहुत ध्यान दे रही है। तभी तो वित्तीय सुधार पर 2007 में रघुराम राजन की अध्यक्षता में बनी कमिटी (Financial Sector Reforms Committee) ने भी ‘निर्णयात्मक स्वामित्व’ की बात की है। यह स्वामित्व सरकार द्वारा गारंटीकृत होगा। इससे खरीद-बिक्री की सहूलियत होगी जिसे भविष्य में कोर्ट में चुनौती दिये जाने की गुजांइश नहीं रहेगी। इस कमिटी ने यह भी सिफारिश की कि भूमि संबंधी रिकॉर्ड ऐसे रखा जाये कि कोई भी, कभी भी उसे देख सके। यह जमीन को रेहन रखने से लेकर ऋण लेने की प्रक्रिया को सुलभ बनायेगा। भूमि उत्पादन के बीमा को भी यह मदद करेगा। इस तरह से पूरा वित्तीय क्षेत्र, बीमा और रियल एस्टेट (FIRE) का व्यवसाय लाभान्वित होगा। साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था में इसी क्षेत्र का शिकंजा है।
इसे आगे बढ़ाने के लिए साम्राज्यवादी वित्तीय महाप्रभुओं ने ‘वित्तीय समावेशन’ को अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर लागू करने की मुहिम छेड़ रखी है। इसके लिए इन्होंने ‘एलायंस फॉर फाइनैनशियल इनक्ल्यूज़न’ नामक संस्था भी बना रखी है जिसका भारतीय रिजर्व बैंक भी मेम्बर है। वित्तीय समावेशन वित्त पूंजी को लाभांवित करता है। रिज़र्व बैंक के द्वारा गठित वित्तीय समावेशन कमिटियों ने भी भूमि रिकॉर्डों के कम्प्यूटरीकरण और फिर ‘निर्णयात्मक स्वामित्व’ की बात की है ताकि संस्थागत ऋण छोटे से छोटे भूमि मालिकों तक पहुंच पाये। इससे उन्हें भी जाल में लेने की मंशा है। भारत जैसे देश में जहां छोटे मालिकों की संस्थागत ऋण तक पहुंच अपेक्षाकृत कमजोर रही है और वे साहूकार पर निर्भर रहे हैं यह बात अच्छी लग सकती है। लेकिन हाल के दशकों में संस्थागत ऋणों में वृद्धि भी हुई है। दूसरी ओर यह बात नहीं भूल जानी चाहिए कि जहां ‘निर्णयात्मक स्वामित्व’ ऋण और मॉर्टगेज को आसान बनायेगा वहीं यह इस स्वामित्व के हस्तांतरण और भूमि की नीलामी को भी सुगम बनायेगा। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए संसदीय कमिटी ने लैण्ड मॉर्टगेज के डेटाबेस पर जोर दिया है ताकि आसानी से पूंजी निवेशक स्थिति को समझ पाये। लैण्ड मार्केट का औपचारिकीकरण ऐसे मॉर्टगेज को प्रोत्साहित करेगा लेकिन खेती की जो स्थिति है उसमें सम्पत्तिहरण को भी त्वरित करेगा। विकसित पूंजीवादी देशों का ऐतिहासिक अनुभव हमें यही बताता है। आज भी अमेरिका में खेती करने वाले छोटे मालिक (कॉरपोरेट के बनिस्पत छोटे) बैंकों से त्रस्त रहते हैं और उनको इस प्रक्रिया में अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता है। जो साहूकार आसानी से आज नहीं कर सकते उसे बहुत ही सरल तरीके से भूमि बाजार के औपचारिकीकरण से किया जा सकता है। यह अधिरचना के क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को सुगम व आसान बनायेगा। आगे की चुनौतियों का भय नहीं रहेगा और साथ ही किससे जमीन लेना है और उस जमीन की अवस्थिति कहां है यह स्पष्ट रहने से मामला आसान बनेगा। इस तरह से बड़ी पूंजी विशेषकर वित्त पूंजी इस पर जोर दे रही है और बिहार का सर्वे भी इसी प्रक्रिया का अंग है। यदि वापस लिये गये तीन कृषि कानून बड़ी पूंजी के पक्ष में कृषि में सम्पत्तिहरण को त्वरित करते और इस क्षेत्र को बड़े पैमाने के पूंजी निवेश के लिए खोल देते तो ऊपर वर्णित मुहिम भी इस प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करेगा चाहे मॉर्टगेज के माध्यम से हो या लैण्ड लीज़िग या फिर भू-सम्पत्ति की बिक्री के माध्यम से।
जहां दूसरी सरकारें भी इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रही थीं कॉरपोरेट पूंजी की चहेती मोदी सरकार इसे त्वरित ढंग से करना चाहती है। तभी तो केन्द्र सरकार इस डिजीटलाइज़ेशन स्कीम के लिये पूरा वित्त वहन कर रही है। याद रहे कि सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने जमीन अधिग्रहण अधिनियम को संशोधित कर बड़ी पूंजी द्वारा जमीन के हस्तगतकरण को सुगम बनाने हेतु भूमिधारकों के हितों को कमजोर करते हुए दो-दो बार अध्यादेश लाये लेकिन संसद में संख्या के अभाव में यह कानून न बन पाया। सरकार तत्पर है कि लैण्ड मार्केट औपचारिक बने और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़े और यह अड़चनों से मुक्त हो। जो सरकार खनन के लिए और दूसरे ऐसे ही कामों के लिए आबादी का जबरन विस्थापन करती आ रही है वह राजनीतिक रूप से सहूलियत के लिए बड़ी आबादी का बाजारीकृत उपायों द्वारा सम्पत्तिहरण करना चाहती है। वैसे तो राज्य के पास “doctrine of eminent domain” है जिसके तहत ”सार्वजनिक उपयोग” के नाम पर वह जमीन अधिग्रहण कर सकता है। यह संविधान में भी जगह पाता है। लेकिन राजनीतिक रूप से हमेशा यह वांछनीय नहीं होता और ऐसे कदम कड़े प्रतिरोध का मसला बन सकते हैं। वैसे तो यह सरकार लगातार जमीन पर लोगों के हक को कमजोर करने की लिए तत्पर रहती है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी कमजोर करने की मंशा रखनेवाली सरकार यदि अधिकारों को सुस्पष्ट करने के नाम पर सर्वे करवा रही है तो हमें इस झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। बिहार में भू-सम्पत्ति की मैपिंग (चौहद्दी, इस्तेमाल, स्वामित्व) को भूमि पर न करके ‘हाइब्रिड’ तरीके से किया जा रहा है जिसे हवाई मैपिंग का कहीं-कहीं जमीनी हकीकत से मिलान कर अंजाम दिया जाता है। जमीन पर इसका न होना इसके प्रमाणिकता पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन काम आनन-फानन में करना है क्योंकि सरकार पर दबाव है कि यह काम सम्पन्न हो ताकि लैण्ड मार्केट स्वच्छंद रूप से काम कर पाये। क्या ऐसे में दावा किया जा सकता है कि सर्वे रैयतों की सहूलियत के लिए हो रहा है?
आज बड़ी पूंजी लगातार तमाम प्राकृतिक संसाधनों को हथिया लेने के लिए दांव चल रही है और लोगों का जीवन दूभर कर रही है। वह चाहे खनन के लिये जंगलों का विनाश हो, स्मार्ट सिटी व झुग्गी झोपड़ी के इलाकों के विकास के नाम पर उन पर कब्जा हो, बंदरगाहों के लिए समुद्री तटों की घेराबंदी हो या फिर इस तरह का सर्वे हो। हर ऐसी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है लोगों का विस्थापन चाहे जंगली इलाकों में रहने वाले प्रभावित आदिवासी हों, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले कामगार हों, समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे हों या फिर ग्रामीण गरीब हों। सब में मुख्यतः लाभांवित होने वाला वर्ग बड़ा पूंजीपति वर्ग ही है। जैसा कि हमने ऊपर बताया है इस सर्वे से तो वित्त पूंजी या साम्राज्यवादियों के हित भी जुड़े हुये हैं। ऐसे में जन अभियान, बिहार जनता से आह्वान करता है कि वह शोषक बड़ी पूंजी के इस वर्ग मंशा को नाकाम करने हेतु संघर्ष को आगे बढ़ाये। प्रगतिशील व रैडिकल लक्ष्यों वाले भूमि सुधार कार्यक्रम पर आधारित लैंड सर्वे के लिए संघर्ष तेज करे। जन अभियान, बिहार सर्वे पर उठे सवालों के मद्देनजर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग करता है। इसके अलावा हम मांग करते हैं कि –
- गरीब परिवार जिस भूमि पर बसे हुए हैं, उसका उन्हें पर्चा दो।
- ग्रामीण गरीबों की बस्तियों को अतिक्रमण हटाने या पर्यावरण के नाम पर उजाड़ना बंद करो।
- सरकार भूमिहीनों को 5 डेसिमल बासगीत जमीन देने का वादा पूरा करो।
- जो भूमि रिकॉर्ड कैथी लिपि में हैं सरकार उन्हें हिन्दी में उपलब्ध कराये।
- जमाबंदी और दूसरे रिकॉर्ड को सरकार अद्यतन करे।
- सरकार वन्य अधिकार कानून, 2006 के साथ छेड़छाड़ नहीं करो और बसे हुए लोगों का हक निबंधित करो।
- जिनके पास जमीन वितरण के तहत मिले हुए पर्चे हैं परंतु जो जमीन पर काबिज नहीं हैं उनका हक बहाल करो।
- सरकार जल, जीवन, हरियाली के नाम पर गरीब बाशिंदों को उजाड़ना बंद करे।
- हदबंदी से फाजिल जमीन की भूमिहीनों के बीच बंदोबस्ती करो।
- भूदान के अंतर्गत प्राप्त सभी भूमि का पूर्ण विवरण सार्वजनिक करो और सरकार उस पर नियंत्रण स्थापित कर उसे भूमिहीनों में बांटे।
- बंद्दोपाध्याय भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करो।