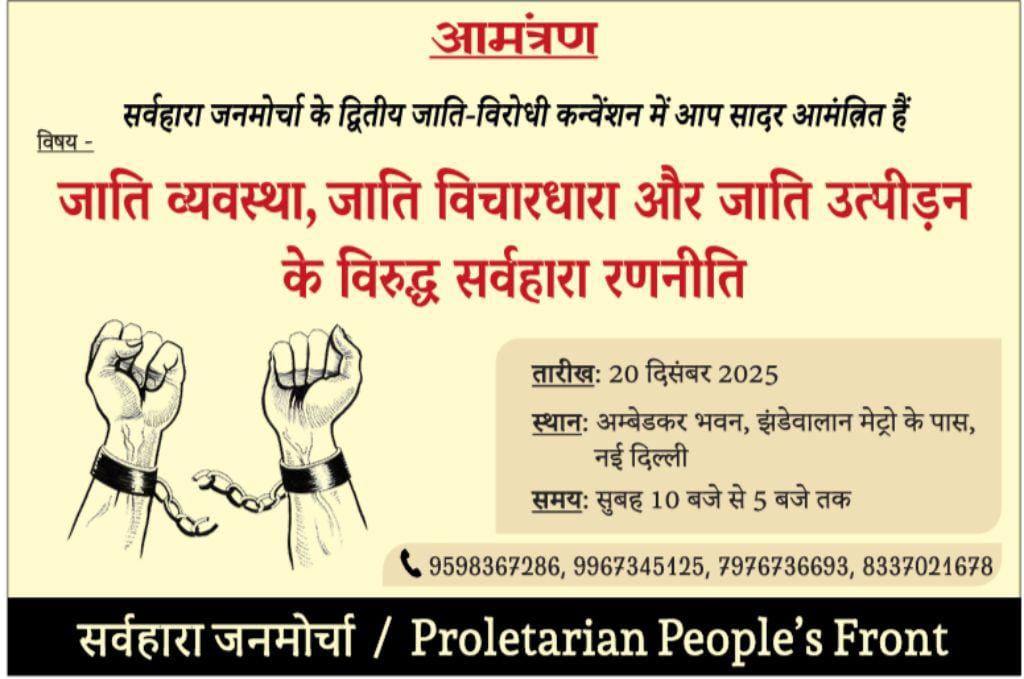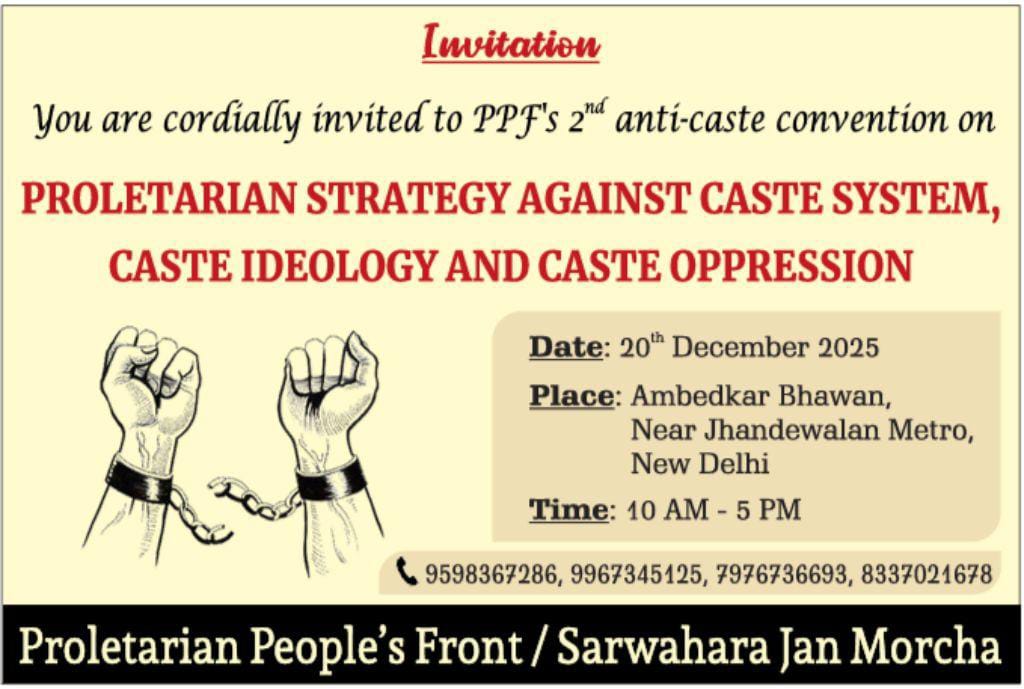वर्ग–जाति के उद्भव एवं उनके उन्मूलन के ऐतिहासिक भौतिकवादी नजरिए में एक योगदान
(20 दिसंबर 2025 को अंबेडकर भवन, दिल्ली में सर्वहारा जन मोर्चा द्वारा आयोजित द्वितीय जाति विरोधी कन्वेंशन में पेश आधार पत्र)
I
जब भी हम इतिहास के सामने यह सवाल रखते हैं कि “वर्ण/जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई” या “इसे कैसे समाप्त किया जाए”, तुरंत हमारे दिमाग में एक दूसरा सवाल कौंध जाता है – मानव इतिहास में इन दोनों में से पहले कौन आया: वर्ग या जाति? और उसके साथ ही सवालों की एक पूरी बौछार लग जाती है: आधुनिक इंसानी प्रजाति कब और कैसे आई, जीवित रही, जीवन यापन किया, भोजन जुटाया और फिर भोजन ही नहीं, अधिशेष भोजन भी उत्पादन करना शुरू किया – जिस अधिशेष के बल पर उन्होंने खुद को सभ्य सामाजिक प्राणी के रूप में संगठित किया और सभ्यता की यात्रा शुरू की? मार्क्स लिखते हैं: “इंसानी इतिहास का पहला आधार, बेशक, जिंदा इंसानों का होना है। इसलिए, सबसे पहले जो बात साबित करनी है, वह है इन लोगों का भौतिक संगठन और बाकी प्रकृति के साथ उनका रिश्ता… (इसलिए*) इतिहास लिखना हमेशा इन प्राकृतिक आधारों और इतिहास के दौरान इंसानों के हस्तक्षेप से उनमें हुए बदलाव से शुरू होना चाहिए।”
इस तरह, इंसानी इतिहास कुछ और नहीं बल्कि इस धरती पर इंसान के जन्म के बाद से इंसान की जिंदगी और उस बाकी प्रकृति के साथ संबंधों में हुए बदलावों की कहानी है, जिसे लाखों सालों में मनुष्यों और उनके भौतिक संगठनों के हस्तक्षेप ने भी बदला है। इसलिए, जाति खत्म करने का काम, एक असल व्यवहारिक क्रांतिकारी काम बनने से पहले, एक कठिन सैद्धांतिक कार्य है – आम तौर पर इंसानी सभ्यता और खास तौर पर भारतीय सभ्यता के विकास की कुंजी को समझने के सही ऐतिहासिक भौतिकवादी नजरिए पर पहुंचने का कार्य। इसके बाद ही वर्ण/जाति व्यवस्था सामने आती है – सही-सही कहें तो, लगभग 1100-1000 BCE में, पहली भारतीय नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता (~1900 BCE) के खत्म होने के लगभग 1000 साल बाद। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम नगरीय लोगों (सिंधु घाटी IVC) के आने के साथ ही पूर्व धार्मिक अनुष्ठानों और पंथों में ढील स्पष्ट दिखती है। पहले के नवपाषाण/ताम्रपाषाण संस्कृति और बाद के वैदिक समाज, दोनों की तुलना में धर्म का प्रभाव काफी कम हुआ था। अनुष्ठान थे, लेकिन वे न तो बहुत विस्तृत थे और न ही हावी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वर्ग अनुष्ठानिक या धार्मिक रूप से जड़ हो गए थे। हमें कोई वर्ण या जाति जैसा जन्म-आधारित, वंशानुगत, वैचारिक रूप से अपरिवर्तनीय पदानुक्रम नहीं मिलता। संक्षेप में, हालाँकि धर्म ने अधिशेष हड़पने वाले अमीर लोगों के अधिकार को सही ठहराने में कुछ भूमिका निभाई, लेकिन राजनीति या सत्तारूढ़ व्यवस्था में इसकी कोई केंद्रीय जगह नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) की एकजुटता, विस्तार और खुशहाली मुख्य रूप से शीर्ष की केंद्रीकृत प्रशासनिक और आर्थिक शक्ति पर निर्भर थी, न कि किसी पुरोहिताई या अनुष्ठानिक वर्ग/जाति व्यवस्था पर।
क्योंकि वर्गीय विभाजन सभ्यता के युग से बहुत पहले का है, इसलिए वर्ण/जाति व्यवस्था वर्ग से बहुत बाद में आई। पुरापाषाण युग से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता (लगभग 3300–1900 BCE) तक के भारतीय इतिहास की करीब से जांच करने पर पता चलता है कि शहरी सभ्यता के आने से बहुत पहले ही वर्गीय विभाजन और गैर-उत्पादकों द्वारा अधिशेष को हस्तगत करना शुरू हो गया था — यह नवपाषाण क्रांति (लगभग 7000–3800 BCE) के बाद के चरणों में ही आरम्भ हो गया था, जो मेहरगढ़ में विकास की तीन अवस्थाओं से मेल खाता है, जो भौगौलिक रूप से इंडस बेसिन (Indus basin) के बहुत करीब था – वह गांव जिसने नवपाषाण क्रांति की सभी अवस्थाएं देखीं और आखिर में 3800 BC के बाद जिसका अपकर्ष या क्षय शुरू हो गया।
जहां तक वर्णों के आगमण की बात है, वे एक बिल्कुल अलग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आए, लगभग 1100–1000 BCE में (जिसका जिक्र सबसे नए ऋग्वेदिक सूक्त, पुरुष-सूक्त, RV 10.90 में किया गया है) – यानी, सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के लगभग एक हजार साल बाद। यह वह समय था जब मध्य एशिया से मैदानी इलाकों से आए अर्ध-खानाबदोश चरवाहे वैदिक आर्य ग्रेटर पंजाब में आए और धीरे-धीरे बिखरी हुई, गांव-आधारित, उत्तर हड़प्पाई खेती-बाड़ी करने वाली आबादी पर अपना राजनीतिक, भाषाई और धार्मिक दबदबा मजबूत किया। शुरुआत के समय, चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय/राजन्य, वैश्य, शूद्र) शुरुआती वर्ग बंटवारे के अलावा कुछ नहीं थे। आज की तरीख में इस पर विद्वानों के बीच कोई गंभीर बहस नहीं बची है, सिवाय इस बचकानी बात के कि वर्ण, जातियां, शूद्र, अछूत या बहिष्कृत, ये सभी अचानक भारतीय सामंतवाद के साथ या उससे ठीक पहले आए क्योंकि उन्हें भारत में विदेशी लाए थे। हालांकि, यह भी सच है कि शुरुआती वर्ग–बंटवारा वर्णों के साथ नहीं आया था, बल्कि वह पहले से ही मौजूद था – यानी उस औपचारिक वर्ण व्यवस्था के आने से भी पहले जिसमें शूद्र भी शामिल थे। ऋग्वैदिक समाज पहले से ही वर्गों में बंटा था – पुरोहित और राजन्य (पुजारी और योद्धा–मुखिया) शासक और अधिशेष हस्तगत करने वालों के तौर पर, और विश (आम लोग) प्राथमिक उत्पादक के साथ–साथ मवेशी चरवाहों के तौर पर कबीलाई ढांचे भी मौजूद थे, लेकिन उसके नीचे उस समय की खेती–बाड़ी वाली अर्थव्यवस्था में मौजूद शुरुआती वर्ग संस्तरीकरण भी मौजूद था।
———————
इरफान हबीब की लिखी हुई बातें (देखें दवैदिकएज) इन बातों को साफ तौर पर साबित करती हैं। यह साबित करने के लिए कि ऋग्वेद के लोगों का जीवन असल में सिर्फ पशुपालन वाला नहीं था, वह न सिर्फ ऋग्वेद का जिक्र करते हैं, बल्कि अलीग्राम (उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान की स्वात घाटी में एक पुरातात्विक साइट) में मिले एक जुते हुए खेत का उदाहरण भी देते हैं, जो लगभग ग्यारहवीं सदी BC का है। वह कहते हैं कि ऋग्वेद के इलाके (सिंधु के मैदान और पश्चिमी सीमा क्षेत्र) में मिली 1500 BC से पूर्व की पुरातात्विक खोजें हमें खेती के बारे में बताती हैं, न कि सिर्फ पशुपालन के बारे में, इसलिए ‘पशुपालन सेक्टर पर ज्यादा जोर देने को सही ठहराना कठिन होगा।’ बल्कि, उनके अनुसार, ‘पशुपालन वाला सेक्टर खेती की जरूरतों की वजह से जरूरी था।’ वह यह भी कहते हैं कि अधिशेष पैदा होता था और उसका हस्तगतकरण भी होता था। जो लोग अधिशेष को हस्तगत करते थे और उसे ‘अपने कब्जे में रखते थे, वे शासक और पुजारी थे – बाद के क्षत्रिय और ब्राह्मण।’ इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि ऋग्वेदिक समाज, वर्णों के आने से पहले भी, वर्गों के आधार पर बंटा हुआ था। ऋग्वेद के एक सूक्त (VIII, 35, 16-18 और 1, 113, 6) के श्लोकों का जिक्र करते हुए, वह साफ कहते हैं कि ‘जो लोग राज करते थे या फायदा उठाते थे और जो सिर्फ मेहनत करते थे, उनके बीच वर्ग का फर्क यहाँ साफ दिखता है।’ समाज के कबीलों में बंटवारे के बारे में (जिसके लिए कभी-कभी जन शब्द का भी इस्तेमाल होता था, जिसका मतलब लोग, यानी people भी होता है; जैसे, पंच जन:, ‘पाँच कबीले’, या यादव-जन, ‘यदु कबीला’। ऋग्वेद हमें अलग-अलग कबीलों के तीस से ज्यादा नाम देता है), वह कहते हैं कि ये कबीले ‘इस सरल वर्गीय ढांचे के अंतर्गत ही लगते हैं।’ कबीले की बनावट पर ज्यादा बात करते हुए, वह आखिर में कहते हैं कि ‘कबीले के अंदर सामाजिक बँटवारा वंश के बजाय वर्ग के आधार पर लगता है।’
लेकिन रामशरण शर्मा इसका खंडन करते हैं, जिनके विचारों को सुवीरा जायसवाल हर मुमकिन तरीके से समर्थन करती हैं। फिर भी, उनकी मिली-जुली बातों से सच प्रकट हो जाता है। मार्क्स की मशहूर बातों को उद्धृत करते हुए कि इंसानों का शिकार जानवरों के शिकार का ही तार्किक विस्तार था रामशरण शर्मा मानते हैं कि ‘कबीलाई सरदारों द्वारा लूट के असमान ‘बंटवारे’ ने ऋग्वैदिक कबीलाई समतावादी लोकाचार को कमजोर कर दिया’ (जायसवाल की ‘कास्ट: ओरिजिन, फंक्शनएंडडाइमेंशनऑफचेंज‘, पेज-139)। वे आगे कहते हैं कि ‘पदानुक्रम भेद था, लेकिन वर्ग भेद नहीं था’ (वही), लेकिन दो वाक्यों के बाद ही, उन्हें यह मानना पड़ा कि ऋग्वैदिक साहित्य के अधुनातन रूप ‘दानस्तुतियों से पता चलता है कि समाज व्यवस्था धीरे-धीरे ज्यादा विभेद की ओर बढ़ रही थी’। यह बताता है कि ‘लूट का एक बड़ा हिस्सा सरदारों और पुजारियों द्वारा हड़पने से एक असमान वितरण व्यवस्था बन गई। ‘इतना ही नहीं, सुवीरा जायसवाल खुद कहती हैं कि “तीन प्रकार के सामाजिक भेदभाव का साफ सबूत ऋग्वेद के मंडल VIII से मिलता है” जिसमें “हम एक त्रिपक्षीय कार्य विभाजन देखते हैं, शायद पदानुक्रम में।” लेकिन सबसे अहम बात वह यह कहती हैं कि – “एक ताकतवर पुरोहित वर्ग का विकास और ब्राह्मण वर्ण का बनना सिर्फ नृजातीय झुकाव का मामला नहीं हो सकता; ज्यादा अधिशेष की मौजूदगी (जो लोगों के खेती में लगे बिना नहीं आ सकती*) और जबरदस्ती हासिल किया गया ख़ाली समय अनुष्ठानों के बढ़ने और ऐसे विशेषज्ञ समूह के बढ़ने के लिए जरूरी शर्तें हैं जो पहले बड़े प्रजनन अनुष्ठानों पर नियंत्रण करते हैं और फिर कुलों, पूर्वजों और देवताओं के बीच मध्यस्थ बन बैठते हैं। इस प्रक्रिया को ऋग्वेद में देखा जा सकता है।” और आखिर में, वह कहती हैं, “ऋग्वेदिक समाज एक सरल समाज था जिसमें पदानुक्रम जन्म से मिली दौलत या हैसियत पर नहीं, बल्कि निजी गुणों और कौशलों पर ज्यादा निर्भर करती थी। हालांकि, ‘जो कामयाबी और अनुभव से मिला’ वह ऋग्वेदिक काल के आखिर तक ‘वंशानुगत और पौराणिक/रीति-रिवाजों पर आधारित’ हो गया, एक ऐसा परिवर्तन जिसका बाद के वैदिक स्रोतों में स्पष्ट प्रमाण मिलता है” – वे यह भी कहती हैं। नतीजा यह कि इरफान हबीब, रामशरण शर्मा, डीडी कोसंबी और सुवीरा जायसवाल लगभग एक ही राय पर सहमत होते दिखते हैं: कबीले के अंदर सामाजिक बँटवारा खानदान के बजाय वर्ग के आधार पर हुआ लगता है; जैसा कि इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं। ऋग्वेद में बालि के कई जिक्र हैं। इन जिक्रों के बारीक अध्ययन से हमें पता चलता है कि बालि एक थोपा हुआ नजराना था, न कि अपनी मर्जी से दिया जाने वाला चढ़ावा। इरफान हबीब लिखते हैं कि “हालांकि, हमें नहीं पता कि यह कैसे लगाया जाता था, और इसे किस तरह से दिया जाता था; ऐसा लगता है कि सिर्फ मवेशी, घोड़े और सोना ही नहीं, बल्कि खेती की पैदावार भी इसका हिस्सा थी।”
———————-
अब, सवाल है, शूद्र कहाँ से और कैसे आए, जिसके बाद वर्ण व्यवस्था वजूद में आई? पराजित मूल आबादी (लगभग 1100–1000 BCE) का बड़ा हिस्सा, जिसमें पहले से ही स्थानीय उत्तर हड़प्पा आबादी के साथ मिल चुके और वहीं बस गए पूर्व-वैदिक आर्य भी शामिल थे, (जिन्हें भी, अनार्यों के साथ-साथ, ऋग्वेद में दास/दस्यु कहा गया है), को शूद्रों के दर्जे तक दबा दिया गया था – यही गुलाम और उत्पादक श्रम, दोनों का मुख्य स्रोत थे। हालाँकि, यह मिलना (assimilation/integration) भी विभेदीकृत था: कुछ हारे हुए ग्रुप ब्राह्मण, तो कुछ क्षत्रिय या वैश्य के रूप में भी शामिल हुए। इस तरह, वर्ण व्यवस्था इसके पहले से मौजूद वर्ग विभाजन पर एक वैचारिक आवरण के तौर पर उभरी। दूसरे शब्दों में, वर्ण पहले से मौजूद वर्गों के ऊपर बने थे। बाद में, शासक तबके (ब्राह्मण और क्षत्रिय) ने अपने प्रभुत्व को अनिश्चितकाल तक बनाए रखने के लिए वर्ण को अनुष्ठानिक और धार्मिक रूप से कठोर बना दिया।कार्य और भूमिकाएं जन्म और आनुवंशिकता द्वारा स्थायी रूप से तय हो गईं; वर्ण वंशावली की दृष्टि से बंद, स्तरीकृत और कठोर हो गए। फिर भी, उत्पादक शक्तियों और वर्ग संबंधों में बदलाव के साथ, इन “कठोर” वर्णों ने भी अपनी वास्तविक भूमिका लगातार बदली। कुछ उदाहरण हैं: पहला, ऊपरी और मध्य गंगा के मैदानों में लौह प्रौद्योगिकी और धान की खेती के आने से, अधिशेष निष्कर्षण बढ़ गया, और इसके साथ ही शूद्र (वैश्यों के साथ) कृषि में प्रत्यक्ष उत्पादक बन गए। इसके पहले शूद्र मुख्य रूप से दास श्रम का स्रोत थे।दूसरा, लौह युग के आने के साथ खेती से बड़े पैमाने पर अधिशेष निकालने से दस्तकारी में विशेषीकरण हुआ और अलग-अलग केंद्रों पर नए शिल्पों का विकास हुआ, जिससे शहरों और लंबी दूरी का व्यापार बढ़ा। इसने बाद में दूसरे शहरीकरण (6ठी-4ठी सदी BCE) की नींव रखी, जिससे कारीगर, व्यापारी और सौदागर वगैरह जैसे नए वर्ग बने। तीसरा, मौर्य साम्राज्य के तहत, जब दूसरा शहरीकरण अपने शिखर पर था, ब्राह्मण ज्यादातर वेतनभोगी सरकारी अफसर बन गए, जबकि क्षत्रिय स्थायी सेना चलाने वाले राजा बन गए। चौथा, अमीर वैश्य पूरे व्यापारी बन गए, जबकि गरीब या कम अमीर और नाकाम लोग तेजी से शूद्र श्रेणी में धकेल दिए गए। पाँचवाँ, शूद्र ज्यादातर निर्भर लेकिन आजाद किसान बन गए। जब बाद के मौर्य काल में टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, तो बड़े पैमाने पर किसानों (ज्यादातर शूद्र) के विद्रोह और टैक्स देने से मना करने की घटना ने साम्राज्य के पतन में काफी मदद की। गुप्त काल से, ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर जमीन देने से उनमें से कई सामंती जमींदार बन गए, जबकि नए क्षेत्रीय राजवंशों ने पुराने क्षत्रिय योद्धा अमीर वर्ग की जगह कुछ हद तक ने ली या उनमें शामिल हो गए। संक्षेप में, पूरे इतिहास में वर्णों (और बाद में उनके अंदर जाति समूहों) के असली आर्थिक काम और वर्ग अंतर्वस्तु, उत्पादक शक्तियों के विकास और उत्पादन संबंधों में बदलाव के अनुसार बदलते रहे – भले ही जन्म–आधारित, अनुष्ठानिक पवित्रता वाले वर्ण पदानुक्रम के वैचारिक आवरण का बार–बार इस्तेमाल नई सच्चाई को स्थिर करने और उसे सही ठहराने के लिए किया गया।
इस प्रकार अब हमारा कार्यभार एक बहुत ठोस रूप ले लेता है: हमें यह जांच करने की जरूरत है और इस जांच के आधार पर, होमो हैबिलिस से लेकर शरीर रचना की दृष्टि से आधुनिक मानव (एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन, AMM) तक मानव प्रजाति की शारीरिक संरचना में विकास की भूमिका का पता लगाना है, साथ ही औजारों के विकास का भी – पहले लाखों वर्षों तक कठोर और अस्थिर पारिस्थितिकी को झेलते हुए प्रकृति से भोजन प्राप्त करने के लिए, और फिर, नवपाषाण क्रांति से लेकर अब तक के भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास में भोजन के उत्पादन के लिए – जिसमें अधिशेष (उत्पादकों की न्यूनतम गुजारे की जरूरत से ज्यादा भोजन) शामिल है। इसमें गैर उत्पादकों द्वारा अधिशेष हस्तगतकरण का सवाल सबसे जरूरी और बुनियादी फैक्टर है – जिसने न सिर्फ वर्गों और वर्ग शासन के उदय को तय किया है, बल्कि उन वर्णों और जातियों के उदय को भी तय किया है जो वर्गों के ऊपर बनी थीं।चूँकि हमें जाति उन्मूलन के सवाल से निपटने के लिए ‘वर्ग’ के साथ ‘जाति’ (या इसके विपरीत) के बहुत ही घनिष्ठ और गतिशील संबंध के संदर्भ में ऐसा करने की जरूरत है, यह निस्संदेह एक परम आवश्यक विषय है।
II
इंसानी इतिहास की वैज्ञानिक पड़ताल से यह साबित हुआ है कि खेती की शुरुआत सभी सभ्यताओं की नींव है; यानी, खेती ही वह बुनियाद है जिस पर सभ्यता का दौर शुरू हुआ। हालांकि, ज्यादा सही कहें तो, सभ्यता के दौर का मतलब ही वर्ग संस्तरीकरण वाली सभ्यता है, और यह तभी शुरू हुआ जब इंसानों ने न सिर्फ खाद्य उत्पादन शुरू किया, बल्कि नियमित रूप से और इतनी मात्रा में अधिशेष खाद्य उत्पादन शुरू किया कि उसके भंडारण की जरूरत पड़ी, ताकि सभ्यता को चलाने के लिए उसका हस्तगतकरण कर केंद्रीकृत इस्तेमाल किया जा सके। भारत में ऐसी भौतिक स्थिति लगभग 3300–2600 BCE के आसपास थी जब सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी जा रही थी। इसी बात को सिद्धांत के हिसाब से कहें तो: जब शुरुआती आधुनिक इंसानों ने न सिर्फ खाद्य उत्पादन शुरू किया, बल्कि अधिशेष उत्पादन शुरू किया, तो उसके साथ ही गैर उत्पादकों या शासक अभिजात्य वर्ग द्वारा उस अधिशेष को हड़पने की व्यवस्था भी आरम्भ हो गई। बाद में उन्होंने या तो जबरदस्ती, या इसे सही ठहराने वाले धार्मिक विश्वासों के जरिए, या दोनों तरह से, हड़पने का अपना यह अधिकार स्थापित कर लिया।
यहां यह ध्यान देना चाहिए कि धर्म के औपचारिक स्वरूप का उदय उन धार्मिक विश्वासों और रीति-रिवाजों से अलग है, जिनकी जड़ें जांगल युग (अपर पुरापाषाण युग) के अज्ञान में हैं। यह किसी भी तरह के दृश्य श्रम विभाजन के शुरू होने से भी पूर्व की चीज है। मौतकेबादक्याहोताहै, इसका जवाब खोजने की जद्दोजहद की शुरुआत असली एनाटॉमिकली आधुनिक इंसान (होमो सेपियंस सेपियंस) के आने के ठीक बाद हो गई थी, जिसका दिमाग, फेफड़े और स्वर रज्जु (वोकल कॉर्ड) आज के हमारे जैसे ही अच्छी तरह से विकसित हो गए थे, और इसलिए उसकी बोलने और सोचने की क्षमता में काफी सुधार हुआ था। आधुनिक जीवविज्ञान, खासकर अपने शरीर की आधुनिक शारीरिक बनावट और कार्यों की कोई जानकारी न होने के कारण, वह मौत के बाद के जीवन और आत्मा के अमर होने के अंधविश्वास में पड़ गया, जिसे उसने मौत से पहले अपने शरीर की हर भावना (दर्द, भूख, प्यास, प्यार, नफरत, वगैरह) का कारण माना। हालाँकि, यह तो बस शुरुआत थी, और इसने भविष्य में धर्म के एक ऐसे भाववादी दर्शन के तौर पर विकास की पहली नींव रखी जो इस जगत की हर चीज के अस्तित्व की व्याख्या करता है। इसी तरह एक धार्मिक पुस्तक होते हुए भी ऋग्वेद भारत में औपचारिक धर्म की बस शुरुआत भर थी। उत्तर वैदिक कृतियों से उपनिषदों तक यह धीरे-धीरे एक औपचारिक धर्म में बदल गया। लब्बोलुबाब यह कि भारतीय संदर्भ में जिसे हम आज धर्म के रूप में जानते हैं, वह अनगिनत अनुष्ठानों पर आधारित धर्म का वह औपचारिक रूप है जो बाद में मनुस्मृति सहित दूसरे धार्मिक साहित्यों के इसके साथ मिलने से बना और जिसने इसे न केवल उपनिषदिक धर्म से अलग बनाया बल्कि सर्वाधिक प्रतिगामी धर्म भी बना दिया।
ऊपर की चर्चा से हम जानते हैं, कि शहरीकरण नए वर्गों को जन्मता और पुराने जड़ीभूत वर्गों और जातियों को गतिशील बनाता है। इसीलिए भारतीय इतिहास के पहले और दूसरे शहरीकरण के दोनों दौर धार्मिक और जातिगत लचीलेपन के जन्म से जुड़े और इसके गवाह रहे हैं। सिंधु सभ्यता में हमें कम धार्मिक अनुष्ठान मिलते हैं; धर्म अभी तक जंतुरूपी (zoomorphic) था, मानवरूपीकृत (anthropomorphic) नहीं बना था। दूसरे शहरीकरण में वर्ण-जड़ता, जन्म के आधार पर ऊँच-नीच और अनुष्ठानों का विरोध बहुत बढ़ा – इसके बावजूद कि अब वर्गों का अस्तित्व और शोषण का तरीका मात्र बदला था।
इसलि जाहिर है, अगर शहरीकरण और सभ्यता का विकास वर्गों के अस्तित्व से रहित हो (जैसे ऐसा समाज जिसमें उत्पादन के साधन पूरी तरह से समाजीकृत हों), तो निश्चित रूप से जाति, जाति व्यवस्था और उन्हें वैध बनाने वाले धर्म का अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन, हम पाते हैं कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया बीच में ही ढह गई – एक बार नहीं बल्कि कई बार। सामंतवाद के उदय तक की बारीक पड़ताल इसकी एक ठोस वजह बताती है: जब भी केंद्रीय नियंत्रण खत्म हुआ, या तो शहरीकरण की रफ्तार कम हो गई या यह पूरी तरह से रुक और खत्म हो गया। हम कमोबेश यही रुझान जारी देखते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश जीत और 1858 में भारत पर ब्रिटिश कब्जे तक शहरीकरण बार-बार उभरता, और ढहता, रहा। ब्रिटिश जीत और आधिपत्य ने जरूर एक अलग तस्वीर पेश की क्योंकि इंग्लैंड तब एक साम्राज्यवादी देश बन गया था और उसने भारत को अपने कच्चा माल का उपांग बना दिया।
अगर हम आज की आधुनिक पूंजीवादी सभ्यता को देखें, तो यह पक्का लगता है कि पूंजीवादी-साम्राज्यवादी उत्पादन पद्धति के अंदरूनी संकटों के कारण यह या तो तबाही की कगार पर है (बढ़ते हुए अंतर-साम्राज्यवादी विरोधाभासों जनित न्यूक्लियर युद्ध की संभावना के कारण) या पूरी तरह से प्रतिगमन के कगार पर है (फासीवाद के उदय के कारण जो जल्द ही समाज को मध्ययुगीन बर्बरता और राजशाही व्यवस्था में वापस ले जाएगा)। फासीवाद के उदय का मतलब आक्रामक युद्ध भी है – देश के अंदर अपने ही लोगों के खिलाफ और देश के बाहर दूसरे (कमजोर) देशों के लोगों के खिलाफ। दूसरे को देशभक्ति बता इसके जरिए पहले को वैध ठहराया जाता है। ये दोनों ही जंग की ओर ले जाते हैं, और अगर सामाजिक व्यवस्था में जल्द ही बदलाव नहीं हुआ तो इन दोनों ही रास्तों से तबाही मुमकिन है।
पूर्व की चर्चा से वापस जुड़ते हुए: एक खास मोड़ पर वर्ग ने वर्णों को जन्म दिया, और उन्हीं वर्गों ने, जो अब पूंजीवादी–साम्राज्यवादी वर्ग के रूप में हैं, इंसानी सभ्यता के पूरी तरह खत्म होने की संभावना को जन्म दिया है। इस तरह जाति को खत्म करने का काम इंसानी सभ्यता को बचाने और उसे लगातार ऐतिहासिक तरक्की के रास्ते पर बनाए रखने के काम से जुड़ जाता है। यहां यह दोनों काम मिलकर एक हो जाते हैं।
दूसरा, आज आधुनिक सभ्यता के समक्ष जो खतरे हैं, वे पहले की सभ्यता के लिए घातक बने खतरों से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। तब, सभ्यता के खत्म होने के बाद भी, उसका आधार – खेती-दस्तकारी या व्यापार – बचा रहा। जो मुख्य रूप से ढहा, वह थी अधिशेष उगाहने की केंद्रीकृत प्रणाली। स्थानीय स्तर पर उत्पादन और खेती से अधिशेष उगाहना/हड़पना जारी रहा। सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के सभी समयों में यही हुआ। देहात की जिंदगी और उसकी वर्ग संरचना की बुनियादी चीजें वैसी ही बनी रहीं। सबसे ताकतवर गैर-आर्य कबीलाई सरदारों में से एक, शंबर, जिसके पास सौ किले (जिन्हें पुरा कहा जाता था, और पत्थर और कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने होते थे) थे, और दूसरे वर्चिन, जो कई फौजी टुकड़ियों का नेतृत्व करते थे, के वर्णन यह बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद और वैदिक समाज की शुरुआत से पहले भी गांव-स्तर की संरचना आरंभिक वर्गीय संरचना थी। यहां यह गौरतलब है कि जहां वर्ग और निजी संपत्ति पहले अधिशेष उत्पादक समाजों के साथ आए, वहीं राज्य – जो ‘वैध‘ हिंसा और प्रादेशिक शासन तंत्र पर एकाधिकार कायम करता है – खास तौर पर शहरी सभ्यता के आने के साथ आया, जिसका सीधा सा कारण यह था कि केंद्रीकृत राज्य नियंत्रण के बिना शहरी सभ्यता का होना और बढ़ना नामुमकिन था।
III
अधिशेष कब्जा करने वाले प्रथम समूह कौन थे? निस्संदेह वे पुजारी और योद्धा वर्ग थे, जिनकी जड़ें उस समय के खेती-बाड़ी करने वाले और पशुपालक जीवन की पारिस्थितिकी में हैं। आबादी का एक छोटा सा हिस्सा – पुजारी और योद्धा – सामाजिक रूप से कबीले के रखवाले और रक्षक के तौर पर उभरे। पुजारी कबीले की आम भलाई के लिए बाहरी एजेंसियों से प्रार्थना करते और गाते थे, जबकि योद्धा कबीले की संपदा बढाने के लिए जंग लड़ते और मवेशी लूटने हेतु हमले करते थे। इसके एवज में दोनों लूट या अधिशेष का बड़ा हिस्सा लेने लगे और इस तरह आबादी के उस बड़े हिस्से पर अपना दबदबा बनाया जो आम लोग थे – उत्पादक या मवेशी पालक या दोनों। यह दुनिया के हर उस हिस्से में हुआ जहाँ आज जैसे इंसान रहते थे और उन्होंने सभ्यता की अपनी यात्रा शुरू की थी।
भारत में ऋग्वैदिक समाज (1500–1100 BCE) में भी ऐसा ही तीन तरह का काम का बँटवारा था: पुजारी, योद्धा और जनसाधारण, जो असल में कबीलाई पदानुक्रम के ढांचे में छिपे शुरुआती वर्ग विभाजन थे। इस बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। दास/दस्यु कबीलों की हार के बाद, और उन्हें गुलाम और साथ ही प्रोडक्टिव मजदूर (शूद्र) की चौथी कैटेगरी के तौर पर वर्ण सिस्टम में शामिल कर लिये जाने के बाद, ऊपर बताया गया शुरुआती वर्ग विभाजन, जो पदानुक्रम के आवरण में छिपा हुआ था, वर्णों के आवरण में छिपे शुरुआती वर्ग विभाजनमें बदल गया, जिसने कुछ ही सदी बाद, तथाकथित समतावादी कबीलाई ढांचे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। यह बात उल्लेखनीय है कि शूद्रों के शामिल हुए बिना और गंगा के ऊपरी व मध्य मैदानों में बड़े पैमाने पर धान के उत्पादन से अधिशेष निकालने की बड़ी संभावना के संदर्भ में शूद्रों को उत्पादक श्रम के एक स्थाई स्रोत में बदलने की गहरी जरूरत के बिना, साथ ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों की हमेशा अपने राज को बनाए रखने की गहरी इच्छा के बिना, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं बन सकती थी। ऊपर बताई गई जरूरत और इससे पैदा हुई इच्छा के मेल से ही वर्ण व्यवस्था शुरू हुई, जिससे शुरू से ही समाज में नफरत और दूरी आई, हालांकि सहभोज और शादी पर रोक बाद में लगी। यह सच है कि वर्णों का सख्त स्तरीकरण और जातियों में इसका और ज्यादा विभेद (जिनकी मुख्य खासियतें काम का खानदानी बँटवारा, सजातीय विवाह और छुआछूत हैं) बाद में शुरू हुआ, लेकिन वे इसलिए शुरू हुए क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ये रुझान शुरू से ही मौजूद थे।
———————
सुवीरा जायसवाल भी यह कहती हैं कि ऐसी कई तरह की राय हैं (जैसे ड्यूमॉन्ट और अंबेडकर की भी) जिनका इस्तेमाल ‘वर्ण व्यवस्था की एक आदर्श तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि शुरू में यह काम का एक खुला, गतिशील बँटवारा था जो बाद में एक बंद अनुभागों वाले पदानुक्रम में पतित हो गया।‘ इसलिए उन्हें ’इसके सही होने की जाँच करने की जरूरत’ गहराई से महसूस होती है। उन्हें यह खास तौर पर इसलिए लगता है क्योंकि ‘इसका असर अछूत जातियों को वर्ण–विभाजित समाज के हाशिये पर रखने पर पड़ता है।‘ वह यहीं नहीं रुकतीं और कहती हैं कि ‘यह महत्वहीन बात नहीं है कि ईसवी युग के पहले दशक की ब्राह्मणवादी कानूनी पुस्तकों के साथ–साथ मिथिला में लिखे गए वर्णरत्नाकर (14वींसदी CE) जैसे मध्ययुगीन ग्रंथों में भी वर्ण और जाति शब्दों का बिना भेद किए इस्तेमाल किया गया है।‘ उन्होंने सही कहा है कि हिंदुओं में जाति का इस्तेमाल, हालांकि यह बाद में बनी, आम तौर पर ‘वर्ण से शुरू होने वाली जाति व्यवस्था के सभी स्तरों‘ के लिए किया जाता है। उनके मुताबिक इसका कारण है कि ‘दोनों श्रेणी को एक ही सिद्धांत पर परिभाषित और चिह्नित किया गया था, यानी वंशानुगत काम, शादी और सहभोज के मामलों में खास अधिकार और पदानुक्रम आधारित सामाजिक स्थिति‘ और इसलिए, वे कहती हैं, ‘मनु भी कहते हैं कि सिर्फ चार जातियां हैं और कोई पांचवीं नहीं है (मनुस्मृति X.4) और पंद्रह निम्न संकर जातियों को पंद्रह वर्ण कहते हैं (ibid. X.31)।‘ उनके अनुसार, ऋग्वेद में ‘वर्ण’ शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल आर्य और दास कबीलों के बीच एक साफफर्क (sharp distinctions) दिखाने के लिए किया गया था। इसलिए, जब उन्होंने हारे हुए दास कबीलों के ज्यादातर लोगों को अपने साथ जोड़कर चार प्रकार की वर्ण-व्यवस्था शुरू की, तो ‘वर्ण’ शब्द का मतलब फिर से साफफर्क(sharp distinctions) था। सुवीरा जायसवाल के शब्दों में, ‘यही शब्द (‘वर्ण‘) बाद के वैदिक काल में उभरते हुए चार तरह के सामाजिक बंटवारे के लिए इस्तेमाल किया गया था ताकि खानदानी आधार पर उनके बंटवारे और अलगाव पर जोर दिया जा सके।‘ हालांकि, सुवीरा जायसवाल यह बताना भूल जाती हैं कि वर्ण व्यवस्था आने से पहले भी, ऋग्वेदिक समाज वर्ग के आधार पर बंटा हुआ था, जिसमें ‘पुजारी और योद्धा–मुखिया‘ मालिकाना हक के तौर पर और ‘विश‘ सीधे उत्पादक और चरवाहे के तौर पर थे। जब वह कहती हैं कि ‘जब तक पुरोहिती का काम, युद्ध या मवेशी पालने जैसे उत्पादक काम वंशानुगत तौर पर तय मौरूसी पेशे नहीं बन गए थे, तब तक उनके लिए वर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था‘, तो वह भूल जाती हैं कि वे अपने आप में वर्ग थे, और इस तरह, मालिकाना हक वाले पुजारी और योद्धा–मुखिया का वर्गीय पूर्वागह रहा होगा, और इस पूर्वाग्रह के आधार पर, कुछ शुरुआती सामाजिक नफरत और दूरी भी रही होगी। लेकिन, वह सही कहती हैं कि ‘ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को वर्ण श्रेणी के तौर पर नहीं बताया गया है और ऐसी व्यवस्था में पुजारी का प्राथमिक स्थान भी शुरुआती चरण में तय नहीं था, जैसा कि ऋग्वेद (I.113.16) में दिखाया गया है’ और ‘वर्ण का स्तर बाद के वैदिक ग्रंथों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसकी पहचान जाति व्यवस्था की तीनों खासियतों – खानदानी काम, श्रेणिगत सामाजिक स्थिति और ‘सामाजिक पदानुक्रम की स्थिरता के लिए’, पहले उच्च विवाह (hypergamy) के व्यवहार से और बाद में अंतर्विवाह के जरिए, स्त्रियों को अधीन व उपकरण बनाये रखने’ से होती है। और इसलिए, आगे वे कहती हैं, ‘इस बात को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की गई है कि पूरी इमारत (वर्ण व्यवस्था*) उत्पादक और मेहनतकश वर्गों के शोषण पर टिकी थी, जिसके लिए पुरोहित वर्ग ने अनगिनत अनुष्ठान बनाए और योद्धा कुलीनों ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया।दोनों समूहों ने वैश्य और शूद्र वर्णों को नियंत्रित रखने के लिए हाथ मिला लिया।‘ (देखें The emergence of Castes and Outcastes, पेज – 8,9)
————————
इस तरह वर्ग न केवल वर्णों से पहले के हैं, बल्कि उनकी पूर्वशर्त भी हैं: वर्ण पहले से मौजूद वर्गों की बुनियाद पर ही बने थे। दूसरी बात, हालांकि शुरुआत में वर्णों के बीच कोई स्पष्ट सीमारेखा नहीं थी, फिर भी सामाजिक प्रतिकर्षण और दूरी तब भी मौजूद थी – और यह स्वाभाविक था। जल्द ही सहभोज और वैवाहिक प्रतिबंध भी आ गए। सुवीरा जायसवाल के अनुसार, लगभग 400 BCE के आसपास, पाणिनि (आमतौर पर जिन्हें चौथी सदी BCE में रखे जाते हैं) उन शूद्रों की बात करते हैं जिन्हें आर्यों के साथ मेलजोल से निकाला या बाहर नहीं किया गया (आर्याणां अनिरवसितानाम II.4.10)। इसका मतलब था कि ऐसे शूद्र भी थे जिन्हें ऐसे मेलजोल से बाहर रखा गया था। उनके टीकाकार पतंजलि ने बाद में बताया कि चांडाल और मृतपा निर्वसित थे, यानी ऐसे शूद्र जो आर्य बस्तियों, गांवों, कस्बों वगैरह में नहीं रहते थे, और उनके खाने के बर्तन स्थाई तौर पर दूषित थे जिन्हें आग से भी शुद्ध नहीं किया जा सकता था (ज्यादा जानकारी के लिए, सुवीरा जायसवाल, दइमर्जेंसऑफकास्ट्सएंडआउटकास्ट्सदेखें)। असल बात यह है कि वर्ण/जाति में सख्ती बाद में आई, लेकिन इसकी बुनियादी विशिष्टताएं – यानी सामाजिक दूरी और विकर्षण/घृणा मुख्य – शुरू से ही मौजूद थे। खासकर शूद्रों के प्रति सामाजिक नफरत और दूरी की प्रवृत्ति – शुरू से ही मौजूद थीं। शायद इसी वजह से, जैसा कि सुवीरा जायसवाल कहती हैं कि ‘वर्ण श्रेणी के अंदर सबसे पहले जाति/कास्ट जैसे उपविभेद उन लोगों में प्रकट हुए गए जिन्हें ब्राह्मणवादी विचारक शूद्र कहते हैं। (वही)
IV
इसी स्थान पर एक और बात की पड़ताल प्राथमिकता पर करने की जरूरत है: स्तेपी एएनआई (Steppe) से आये आर्यों के भारत आने से वैदिक कर्मकांड वाला धर्म और वर्ण व्यवस्था क्यों बनी? सुवीरा जायसवाल के शब्दों में: वह कौन सी प्रक्रिया थी जिससे सामाजिक स्थिति की सही पहचान और संस्थागतकरण हुआ, उनका वर्ण श्रेणियों में क्रिस्टलीकरण (रवाकरण) हुआ? और यूरोप व मध्य एशिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ?
पहले सवाल का जवाब देने के लिए हम डीडी कोसंबी के शोध का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका मानना था कि यह ब्राह्मण वर्ण था जिसका गोत्र संगठन ‘आर्य पुरोहितों और उत्तर सिंधु संस्कृति के रीति-रिवाजों की दृष्टि से श्रेष्ठ पुरोहितों के बीच अंतःक्रिया के नतीजे में’ सबसे पहले विकसित हुआ, जबकि हड़प्पा संस्कृति के बचे हुए लोग मिले-जुले आर्य समाज में अलग-अलग स्तर पर शामिल हो गए, जिससे चार-भागों वाला वर्ण ढाँचा विकसित हुआ। सबसे अहम था हड़प्पा पुरोहितों का सम्मिश्रण, जिसमें पूर्व-आर्य पुरोहितों के छोटे समूह विजयी आर्य कबीला समूह में शामिल हो गए और उन्हें अपनी पुरोहिती सेवा देने लगे। इन मिश्रित हुए पुरोहितों ने अब तक क्षत्रियों के साथ मिले जुले मूल वैदिक पुरोहितों को भी बदल डाला। इसने क्षत्रिय एलीट से इनके अलगाव को तेज कर दिया। यह एक ढांचागत विकास था जो दास/शूद्र जाति के बनने के साथ-साथ हुआ और इससे सबसे पहले ब्राह्मणों में अंतर्विवाह शुरू हुये। खानाबदोश चरवाहे आर्यों में व्यक्तिगत संपत्ति पर्याप्त विकसित नहीं हुई थी, लेकिन अब जब हड़प्पा की विजित कृषक आबादी, यानी खेती करने वाले लोग (जिन्हें कोसंबी ने दास बताया था) विजेता कबीलों में मिलकर एक अलग समूह बना, तो निजी संपत्ति आर्य लोगों की जिंदगी का भी हिस्सा बन गई। इस तरह आर्यों और गैर-आर्यों के बीच एकीकरण हुआ और दास/शूद्र वर्ण की शुरुआत हुई, और एक अंतर्विवाह आधारित जाति व्यवस्था अस्तित्व में आई। (जायसवाल की ‘कास्ट: ओरिजिन, फंक्शन एंड डाइमेंशन ऑफचेंज‘, पेज-154, 155)
हालांकि, यहां अभी दूसरे सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है: स्तेपी से आए आर्यों के यूरोप और मध्य एशिया में आप्रवास का वैसा ही नतीजा क्यों नहीं निकला? असल में, दोनों सवालों के असली जवाब पारिस्थितिकी के साथ-साथ उन इलाकों के तत्कालीन ठोस ऐतिहासिक खास हालात में हैं।
यह सच है कि ये स्तेपी से निकले आर्य कबीले यूरोप और मध्य एशिया (बैक्ट्रिया-मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स या BMAC) भी गए, लेकिन उन्होंने वहां कोई अति अनुष्ठानिक धर्म और उससे जुड़ा वर्ण सिस्टम नहीं बनाया। यूरोप में, उनके आने के समय, घने नवपाषाणकालीन किसान समुदाय थे जो जंगल/नदी वाले समशीतोष्ण इलाकों में रहते थे। अप्रवासियों ने यहां बड़े पैमाने पर जेनेटिक प्रतिस्थापन किया और वे तेजी से स्थानीय खेतिहर समुदायों में घुल-मिल गए – वही जो भारत की और आर्यों के अप्रवास की प्रथम लहर में हुआ।इससे पुरोहितों का एकाधिकार या बड़े गुलाम एवं मेहनतकश समूह के तौर पर जन्म से बने चौथे वर्ण (शूद्र) की जरूरत खत्म हो गई। इसका नतीजा था अस्थिर कबीलाई ऊँच-नीच (सेल्ट्स, जर्मन, वगैरह), जिसने बाद में ईसाई धर्म के तहत यूरोपीय सामंतवाद को जन्म दिया।
मध्य एशिया में, स्तेपी घुमंतू या अर्ध-घुमंतू समूह BMAC (बैक्ट्रिया-मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स) के शहरी लोगों के साथ मिल गए, इसलिए स्थानीय पुजारियों की परंपराएँ (शुरुआती जोरोस्ट्रियन) और कबीलों का प्रवाह अबाध बना रहा। इसके अलावा, भारत के उलट, वहाँ खेती से हासिल होने वाले अधिशेष में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई (न यूरोप न मध्य एशिया में) जिसके लिए वहां अनुष्ठानिक वर्ण व्यवस्था के नाम पर खेती करने वाले और मेहनतकश वैश्य व शुद्र वर्गों पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण की जरूरत हो। इसलिए वहाँ वर्ण-शैली की सोच पैदा नहीं हुई।
लेकिन जब वे भारतीय उपमहाद्वीप में आए तो उन्हें एक बिल्कुल अलग स्थिति का सामना करना पड़ा: यहां सिंधु घाटी नगरी सभ्यता के ढहने के पश्चात की खेती-बाड़ी करने वाली गाँव आधारित आबादी मौजूद थी जो पूरी तरह से विखंडित, अलग-थलग और बिखरी हुई थी। इसके अलावा, अप्रवास की यह वैदिक आर्य लहर मुख्यतः पुरुषों का आप्रवास था जिसकी भेंट एक बहुत बड़े स्थानीय बिखरे समूह से हुई – और एक छोटा सा एलीट वर्ग बहुत बड़ी आबादी पर राज करने में सफल रहा। इसके अतिरिक्त जल्द ही लौह युग के औजारों (1000–700 BCE) ने धान की खेती में इतना बड़े अधिशेष के उत्पादन की संभावना व क्षमता विकसित कर दी जिसके सामने यूरोप या मध्य एशिया में जो कुछ था, वह बहुत बौना पड़ गया। यहाँ के लाखों नए उत्पादकों को नियंत्रित करने के लिए, साथ ही पूरे उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक झंडे के नीचे लाने हेतु, स्तेपी से निकले इस एलीट वर्ग ने, जिनका एक बड़ा हिस्सा पूर्व-वैदिक उत्तर हड़प्पा संस्कृति का था, अपने कबीलाई पुरोहितों को एक खानदानी संस्था में बदल दिया और चौथे वर्ण, जन्म पर आधारित पदानुक्रम, बहुत ज्यादा कर्मकांड वाला वैदिक धर्म तथा अंतर्विवाह का आविष्कार किया।
V
इस तरह वर्ग, निजी संपत्ति और राज्य इंसानी इतिहास में एक के बाद एक आए, जिनका आधार, एक बार फिर से दोहराएं तो, खेती की शुरुआत से निर्मित नींव थी। अगर हम खुद को प्राचीन काल तक ही सीमित रखें, तो हम इसे मुख्य रूप से दो चरणों में होते हुए देख सकते हैं। पहला चरण “फर्स्ट इंडियंस” – प्राचीन पूर्वज दक्षिण भारतीयों (Ancient Ancestral South Indians – AASI) का है, जो लगभग 65,000 साल पहले शिकारी-संग्रहकर्ता के तौर पर भारत आए थे – जिन्होंने नवपाषाण क्रांति (7000 BCE में मेहरगढ़ में) शुरू की, ईरानी किसानों (4700–3000 BCE, सिंधु घाटी सभ्यता में 50–70% वंश) के साथ मिले और पहली बार सिंधु बेसिन (3300–1900 BCE) केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शहरीकरण और नगरीकरण की शुरुआत की।
दूसरा चरण स्तेपी से निकले इंडो-आर्यन बोलने वाले वैदिक कबीलों के 1900-1500 BCE के कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप में आप्रवास से जुड़ा है। वैदिक आर्य, जो आर्य आप्रवास की बाद की लहरों में, लगभग 1500 BC में आए, जबकि पूर्व-वैदिक आर्य, जो आर्य आप्रवास की पहली लहर में, लगभग 1900 BCE में आए, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता पहले से ही खंडहर हो चुकी थी, और उत्तर हड़प्पा आबादी (कब्रिस्तान H, झुकर कल्चर) के साथ मिल एकाकार हो गए। इन आर्य समूहों ने वैदिक धर्म (~1500 BCE) की स्थापना की, और दस राजाओं के युद्ध (1400–1200 BCE) जैसे टकरावों के जरिए एकीकृत हुए, जिसमें भरत कबीलों ने दबदबे के लिए आर्य (पुरु, अनु) और गैर-आर्य (दास/दस्यु/पाणि) के दुश्मन गठबंधन को हराया – पहले पंजाब में ~1000 BCE तक, और बाद में ऊपरी और बीच के गंगा के मैदानों में धीरे-धीरे पूरब की ओर बढ़कर, यानी ~1000 से ~800 BCE तक इन इलाकों में फैलते हुए।
लोहे के औजारों (~1000–700 BCE) ने खेती और अधिशेष को बढ़ावा दिया। इससे जनपदों (800–600 BCE) और महाजनपदों (600–300 BCE) की नींव पड़ी, जहाँ प्रादेशिक राजा (territorial kings) और उनके तहत, मालिकाना हक का एक सामूदायिक तरीका (यह कबीलाई तरीके से निकला था जो ऊपरी और बीच के गंगा के मैदान में धान के बड़े पैमाने पर अधिशेष उत्पादन को संभाल नहीं पा रहा था और खेती करने वाली लाखों की नई आबादी पर नियंत्रण की एक व्यवस्था की जरूरत पैदा कर रहा था) सामने आया और इस अधिशेष से हासिल किए गए संसाधनों द्वारा ही दस्तकारी/व्यापार के विभिन्न केंद्रों का निर्माण हुआ। इसी ने भारत में शहरीकरण (600–300 BCE) के दूसरे दौर को पैदा किया।
सिंधु घाटी सभ्यता जैसे केंद्रीकृत प्रशासन वाले मौर्य साम्राज्य (321–185 BCE), जिसमें धम्म का संचार भी था, ने लगभग 185 BCE में अपने पतन के पूर्व इसका इस्तेमाल शहरीकरण के शिखर पर पहुंचने के लिए किया। इसके बाद दूसरा शहरीकरण भी धीरे-धीरे विलुप्त हो गया। शहरीकरण का यह दौर बौद्ध और जैन धर्म के जन्म और प्रसार के सांयोंगिक था। यह कई वैचारिक कड़ियों को जोड़ता है: शहरीकरण पुराने और नए वर्गों की बढ़ती गतिशीलता के लिए भौतिक आधार बनाता है, जिससे वर्ण और धार्मिक लचीलेपन के लिए जगह मिलती है और जड़ीभूत वर्ण/जाति व्यवस्था में कुछ हलचल होती है, जिससे एक भूचाल पैदा होता है। वर्ण/जाति के इतिहास की आगे की यात्रा को समझने के दौरान इस पर ध्यान देना चाहिए। यह हमारी इस बात से भी जुड़ता है कि शहरीकरण का जारी रहना या वृद्धि करना शीर्ष पर सत्ता के केंद्रीकरण या केंद्रीकृत योजना के बिना नहीं हो सकता था।
फिर कुषाणकालीन केंद्रीकरण के दौर में व्यापार में तेजी आई। हमें कुषाण और सातवाहन सोने और चांदी के सिक्कों से बहुत ज्यादा व्यवसायिक दौलत की मौजूदगी दिखती है, लेकिन यह केंद्रीकृत कराधान से मुक्त रही। इसलिए इसने शाही खजाने में बहुत कम योगदान दिया जिससे शहरीकरण को आगे बढ़ाया जा सकता। इसके बजाय, पहली सदी CE से ब्राह्मणों और बौद्ध मठों दोनों को धार्मिक टैक्स-मुक्त जमीन-अनुदान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। जमीन एक बार अनुदान में दी गई तो अपने भू-राजस्व सहित शाही खजाने से भी अलग हो जाती थी। इस तरह, इसके बाद के काल में वि-शहरीकरण या वि-नगरीकरण आम बात हो गई।
जब चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध (~320 CE) में सत्ता संभाली, तब उन्हें विरासत में खाली खजाना और कर-मुक्त ब्राह्मण गांवों से भरा देहाती इलाका मिला था। उनके बेटे समुद्रगुप्त (335–375 CE) ने खजाना भरने के लिए बड़े युद्ध अभियान चलाने का पुराना शाही मॉडल आजमाया, लेकिन वह असफल हुए। जब चंद्रगुप्त द्वितीय (375–415 CE) गद्दी पर बैठे, तब तक स्वर्णिम गुप्त साम्राज्य का अंत हो चुका था। उन्हें सामंती व्यवस्था (चल रहे अपने आप होने वाले विकेंद्रीकरण की जगह संस्थागत विकेंद्रीकरण) शुरू करना पड़ा, जिसमें अधीनस्थ राजा स्थानीय राजस्व के अधिकारी सामंत बन गए। इसके अलावा उन्होंने ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को भू अनुदानों में तेजी लाई और प्रांतों के लिए वंशानुगत गवर्नर और जिलों के लिए जिला अधिकारी बनाए। ये पद भी छोटे राज्यों में बदल गए।
इस समय में हुए इन सभी घटनाक्रमों ने “स्वर्णिम गुप्त साम्राज्य” को सामंतों के एक समूह में बदल दिया, जो गुप्त राजगद्दी के प्रति नाम के ही वफादार थे। 450 CE के बाद हूणों के हमलों के समय सामंतों ने वफादारी बदल ली या खुद के लिए लड़े। 550 CE तक गुप्त साम्राज्य परस्पर लड़ने वाले क्षेत्रीय सामंती राज्यों की प्रणाली में बदल गया – अलग-अलग तरह के सामंतों और अनुदान प्राप्तों का एक ढीला-ढाला राज। इस तरह भारतीय सामंतवाद का जन्म हुआ। साम्राज्यों के अधीन स्वामित्व के पुराने सामुदायिक स्वामित्व पद्धति की जगह सामंती निजी संपत्ति आधारित सामंती स्वामित्व के तरीके ने ले ली, जिसका नतीजा यह हुआ कि शहरीकरण बहुत लंबे समय के लिए पीछे धकेल दिया गया। कहने की जरूरत नहीं कि पुराने शहरी केंद्र भी खत्म हो गए।
मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के पतन तक तथा इसके बाद सामंतवाद के जन्म तक की लगभग 700 सालों की यात्रा के साथ ही ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया ने भी जन्म लिया, जिसकी शुरूआत हालांकि शुंग वंश से ही हो चुकी थी – जो मौर्यों का लगभग सीधा उत्तराधिकारी था। ब्राह्मण और मनुस्मृति जैसे उत्तर-वैदिक काल के बाद के ब्राह्मणवादी साहित्य से पता चलता है कि अलग-अलग तरह के वर्ण-संस्तर एक बार फिर से जिंदा ही नहीं हावी हो गए।
आइए, विभिन्न बिंदुओं को जोड़ने वाली कड़ियों की फिर से पुनरावृत्ति करें।
उत्तर वैदिक काल (1000–700 BCE) में वर्ण की सख्ती का असली आधार ऊपरी और बीच के गंगा के बाढ के मैदानों में बड़े पैमाने पर धान की खेती थी, जिसने पुरानी कबीलाई नियंत्रण प्रणाली (पुजारी–योद्धा–आम लोग) को खत्म कर दिया। इसकी वैचारिक प्रतिक्रिया अधिशेष निष्कर्षण के लिए एक स्थायी विशाल श्रम बल के रूप में शूद्रों की स्थापना था – जिसका उल्लेख पहली बार नवीनतम ऋग्वेदिक सूक्त (आरवी 10.90, ~1100-1000 ईसा पूर्व) में किया गया है। तदनुसार, ब्राह्मण ग्रंथों (शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ~900-700 ईसा पूर्व) ने ब्राह्मणों को “पृथ्वी पर देवता” घोषित किया, सजातीय विवाह का आदेश दिया, शूद्रों को वैदिक अध्ययन से मना किया; धर्म-सूत्रों (700-500 ईसा पूर्व) ने जन्म से व्यवसाय तय किया और वर्ण के अनुसार दंड निर्धारित किए (उदाहरण के लिए, यदि कोई शूद्र वेद का पाठ करता है तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डालना)। वर्ण जन्म-आधारित, पदानुक्रमिक और अधिकाधिक कठोर हो गए; खेती में भारी बढ़ोतरी के साथ, अंतर्विवाह आधारित जातियां बढ़ने लगीं।
इसके विरोध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में एक विचारधारात्मक चुनौती खड़ी हुई, जिसका भौतिक आधार सोलह महाजनपदों के तहत दूसरा शहरीकरण था। नए शहर (राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र) बने, व्यापार बढ़ा, और नए सामाजिक समूह (गहपति, श्रेणी व्यापारी, कारीगर) सामने आए जो पुराने चार-वर्ण के खांचों में फिट नहीं होते थे। दोनों धर्मों ने जन्म के आधार पर पदानुक्रम को खुले तौर पर खारिज कर दिया। बुद्ध ने कहा: “कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से बहिष्कृत नहीं होता; सिर्फ कर्मों से…” (वासेठ सुत्त)। महावीर ने शूद्रों और महिलाओं को अपने संप्रदाय में स्वीकार किया। शहरी राजाओं को पवित्रता की नहीं, बल्कि राजस्व की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण गांवों के बजाय बौद्ध/जैन साधुओं और व्यापारियों को बढ़ावा दिया। अशोक (268–232 BCE) के काल में यह जवाबी हमला अपने चरम पर था: महंगे ब्राह्मण रीति-रिवाजों का मजाक उड़ाया गया (रॉक एडिक्ट 9), अहिंसा और सभी संप्रदायों की बराबरी की तारीफ की गई (रॉक एडिक्ट 13), राजकीय धन से हजारों स्तूप और मठ बनाए गए। ब्राह्मणों को ज्यादातर किनारे कर दिया गया। वर्ण/जाति का क्रम बहुत कमजोर हो गया था – खासकर केंद्रीय शाही क्षेत्र में जहाँ शहरी इलाके ज्यादा विस्तृत थे और कई शूद्र किसान और कारीगर गहपति बन गए थे। फिर भी, समाज का बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों के असर में रहा; बौद्ध धर्म ने गांवों में ब्राह्मणों को अधिशेष हड़पने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा, बौद्ध धर्म का कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, और इसके लिए जरूरी मठवासी जीवन, उत्पादक ग्रामीणों द्वारा नहीं अपनाया जा सकता था। पौराणिक ब्राह्मणवाद ने कर्म-निर्वाण अवधारणा को अपना लिया, भक्तिवाद (भक्ति, अवतार, मंदिर) की नकल की और जाति को बनाए रखा।
प्रतिक्रिया शुंगों के समय शुरू हुई और विदेशी हमलावरों (शक, कुषाण) के समय भी जारी रही, जिन्होंने कराधान मुक्त जमीन-अनुदान के बदले स्थानीय सरदारों और ब्राह्मणों से गठबंधन किया। मनुस्मृति (200 BCE–200 CE) वर्ण/जाति का सबसे कड़ा कवच बन गई: शूद्र सिर्फ द्विजों की सेवा के लिए हैं (2.31); मिली-जुली जातियों को दर्जनों अपमानजनक कामों के साथ सूचीबद्ध किया गया; राजा का पहला काम वर्ण-धर्म को बनाए रखना है (7.35, 8.410–418)। सातवाहनों (100 CE) के समय जमीन-अनुदान की एक नई लहर शुरू हुई; कुषाण शासक खुद को “देवपुत्र” कहते थे और वैधता हासिल करने हेतु ब्राह्मणों को भारी अनुदान देते थे। जीनोमिक अध्ययनों (2019–2025) से पता चलता है कि लगभग 100 CE के बाद बहिर्विवाह में बहुत ज्यादा गिरावट आई, अंतर्विवाह नियम बन गया और जातियाँ – जिसमें अछूत/बहिष्कृत समूह भी शामिल थे – पूरी तरह से जड़ीभूत हो गईं।
गुप्तों के बाद बनी सामंती व्यवस्था 1206 CE के तुर्क हमलों तक चली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान घोषित किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। राजपूत राज्यों को खत्म कर दिया गया या उन्हें कर चुकाने वाले अधीनस्थ में बदल दिया गया; नई भू राजस्व प्रणाली ने खजाने को भर दिया क्योंकि जीते हुए इलाके में कोई खानदानी सामंत या कर मुक्त ब्राह्मण गाँव नहीं थे। यह पहले से अलग प्रतीत होता था, फिर भी जाति व्यवस्था वैसी ही रही – नए शासकों ने और भी ज्यादा अधिशेष वसूला (खराज अक्सर पुराने दौर के 1/6 भाग से ज्यादा होता था) और कभी–कभी शूद्र किसानों को और भी दबाने के लिए ब्राह्मणवाद का इस्तेमाल भी किया। लेकिन दूसरी तरफ, केंद्रीकरण से शहरीकरण और व्यापार में तेजी आई (दिल्ली, लाहौर, मुल्तान पाटलिपुत्र के दौर से अब तक के किसी भी शहर से बड़े हो गए), और शहरी कारीगरों और व्यापारियों को गतिशीलता मिली, लेकिन गाँवों का टैक्स का बोझ पुराने सामंती निजाम से भी बदतर होता गया।
1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य (1526–1707) की स्थापना की – यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जमीन से राजस्व वसूलने वाला सर्वाधिक केंद्रीकृत राज्य था। औरंगजेब के समय तक इसका राजस्व उस समय के इंग्लैंड और फ्रांस की कुल राष्ट्रीय आय के बराबर हो गया था। पुराने जमींदारों को अस्थाई ठेके वाले राज्य नियुक्त राजस्व कलेक्टर बना दिया गया; वसूली में असफलता अर्थात् कमी का मतलब था हटाया जाना और दंड। उनका कानूनी मुनाफा सिर्फ 10-15% था। नगदी का जाल बड़े पैमाने पर गाँवों में फैल गया – किसान चाँदी के रुपये चुकाने के लिए अनाज बेचते थे। इस तरह व्यापार और दस्तकारी में तेजी आई और देहात के किसान इससे जुड़ते गये, शहरी मजदूरी बढ़ी, कारीगरों के समूह अमीर हुए। लाहौर, आगरा, सूरत, ढाका, मछलीपट्टनम बड़े मैन्युफैक्चरिंग शहर बन गए। अकेले बंगाल हर साल लाखों चाँदी के रुपये के कपड़े निर्यात करता था। शहरी मजदूरी बढ़ी, कारीगरों के समूह अमीर हुए, और जहाँ भी नगदी इकॉनमी पहुँची, वहाँ गाँव की सख़्त जजमानी प्रणाली (पुराने सामंती जमाने का जाति-आधारित काम का बँटवारा) टूटने लगा। अगर यह प्रक्रिया बिना रुके चलती रहती, तो पुरानी सामंती जाति-व्यवस्था निश्चित रूप से पण्य या माल उत्पादन (commodity production) के समुद्र में डूब गई होती, ऐसा सोंचा जा सकता है।
लेकिन प्लासी (1757) में विजय के बाद 1857 तक के काल में अंग्रेजों ने इसे इरादतन उलट दिया। स्थाई बंदोबस्त (1793) ने राजस्व ठेकेदारों को वंशानुगत निजी जमींदारों में बदल दिया जो असीमित लगान वसूल सकते थे। देसी उद्योग खत्म हो गए, लाखों कारीगरों को जीविका हेतु वापस जमीन की ओर धकेल दिया गया, वि-औद्योगिकरण पूरा हो गया, जाति फिर से जड़ बन गई। अंग्रेजों ने सात बार जाति जनगणना (1871–1931) की, जिससे अब तक की परिवर्तनशील जातियां कठोर, सुगणित (enumerated) अखिल भारतीय जातियों में बदल गईं। फिर भी, अपने लिए भारत की संपदा के बेहतर निकास हेतु, उन्होंने रेलवे, बंदरगाह और कोयला खदानें बनाईं।पहली आधुनिक फैक्ट्रियां बॉम्बे, कानपुर और जमशेदपुर में लगीं। 1940 के दशक तक, भारत में एक छोटा लेकिन असली औद्योगिक सर्वहारा बन चुका था — संकेंद्रित, अनुशासित, और संगठित होता हुआ। इस तरह जाति व्यवस्था पर आखिरी हमले के लिए जरूरी वस्तुगत और मनोगत कारक अस्तित्व में आ गए थे।
VI
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए चले राष्ट्रीय आंदोलन ने कुछ समय के लिए ही सही लेकिन लाखों लोगों को जातियों के तौर पर नहीं, बल्कि ‘भारतीयों’ के तौर पर एकजुट किया – रेलवे कर्मचारी, जूट-मिल मजदूर, लगान चुकाने से इंकार करने वाले किसान, और बॉयकॉट करने वाले छात्र, सभी जाति से भी ज्यादा मजबूत एकता में बंधने लगे। एकता की यह भावना अपने आप में जाति व्यवस्था पर एक हमला थी। डॉ अंबेडकर ने इसी वक्त संपूर्ण जाति विनाश का झंडा उठाया।
लेकिन, आजादी के बाद के दिनों के घटनाक्रम ने उस उम्मीद को तोड़ दिया। “जमीन जोतने वाले को” का जोरदार नारा जमींदार व बुर्जुआ समर्थक अधूरे “भूमि-सुधारों” के नीचे दबा दिया गया; 70-80% जमीन पुराने ‘ऊँची’ जाति और धनी किसान अभिजात्य के पास ही रही। शूद्र और दलित किसान मजदूर या बटाईदार ही रहे। छुआछूत पर कागजी पाबंदी लगा दी गई (आर्टिकल 17), लेकिन नीचे से उत्पादन संबंधों में कोई मौलिक बदलाव नहीं आया। आरक्षण ने एक छोटी सी परत को जरूर अमीर बनाया किंतु ज्यादातर लोग भूमिहीन, कर्ज में डूबे, और अनुष्ठानिक उत्पीड़ित ही बने रहे।
बंटवारे के सांप्रदायिक दंगों, जो बहुत जगह जिन्ना की मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और RSS द्वारा किए गए, में 10-15 लाख लोग मारे गए। फिर भी ये न सिर्फ छुट्टे रहे, बल्कि आजादी के बाद नेहरू की पहली कैबिनेट में आरएसएस ने अपने एक आदमी को भी जगह दिला दी। नेहरू के जमाने में उन्हीं पुराने जमींदारों वाले आधार पर स्टील मिलें बनीं और हरित क्रांति से फला-फूला एक नया अमीर किसान वर्ग तैयार हुआ। तेलंगाना (1946–51) और नक्सलबाड़ी (1967) ने इस दुनिया को नीचे से उलटने की कोशिश की, लेकिन दोनों खून में डुबा दिए गए। 1991 में, जनता के साथ यह धोखा चरम पर पहुँच गया। मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीतियां लाकर बड़े इजारेदारों और वित्तीय पूंजी के धन्नासेठों के लिए मुनाफे के दरवाजे खोल दिए: खरबपति कई गुना बढ़ गए तो झुग्गी बस्तियां भी चौतरफा फैलती गईं, नियमित नौकरियाँ गायब हो गईं, और ग्रामीण दलित गरीब और भी कुचले गए।
2014 में हिंदुत्व के साथ गठबंधन में इजारेदार वित्तीय पूंजी का आखिरी हमला हुआ, जो अब तक जारी है। एक नया ब्लॉक – पुराना ‘ऊँची जाति’ अभिजात्य और पिछड़ों-अति पिछड़ों के अमीर हिस्से, यहाँ तक कि चंद दलित और आदिवासी समुदायों के पूंजीवादी संस्तर भी – मुसलमानों, भूमिहीन मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, मेहनतकश किसानों और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के खिलाफ, खुद जनतंत्र के खिलाफ, फासिस्टों के साथ एकजुट हो – नए शासक सामाजिक गठजोड़ के तौर पर सामने आये हैं।
दूसरे शब्दों में, जाति की सोच अब नए तरह के सामाजिक विलय (fusion) के माध्यम से काम करती है।जुल्म करने वाले और दबे–कुचले समुदायों के अमीर तबके अब मुनाफे की मेज पर एक साथ ही बैठते हैं; जब भौतिक हित एक साथ आते हैं, तो भिन्न जाति मूल के पूंजीपति एक नए जाति ब्लॉक में बदल जाते हैं। आज का “हिंदू राष्ट्र” प्रोजेक्ट ऐसे सम्मिलन को गढ़ने की सबसे नई भट्टी है जिसमें तपा कर मोदी का शासन और RSS एक फौलादी फासीवादी पिंजरा बना रहे हैं।
किंतु इसे तोड़ने वाली एकमात्र ताकत उन्हीं ब्रिटिश रेलवे वर्कशॉप और कॉटन मिलों में पैदा हुई शक्ति है, जिनकी पांचवीं पीढ़ी – ज्यादातर दबी-कुचली जातियों से – आज असंगठित सेक्टर, निर्माण साइटों, खेतों और बस्तियों में बहुत कम या बिना किसी नियमित आय के हाड़तोड़ मेहनत कर रही है। तथाकथित ऊंची जाति मूल के, और दूसरे धर्मों के सर्वहाराओं के साथ मिलकर, असंगठित सेक्टर या यह आधुनिक सर्वहारा आज अपने-आपको एक बहु-जाति, बहु-धार्मिक क्रांतिकारी सर्वहारा में बदल रहा है। मोनोपॉली वित्तीय पूंजी की जबरदस्त लूट ने सभी जातियों के गरीब और निम्न-मध्य वर्ग को इतना हताश कर दिया है कि जातिगत नफरत को लगातार बढ़ावा देने के बावजूद एक नया बंटवारा (हर जाति के अंदर गरीब बनाम अमीर) और एक नया मेल (सभी जातियों के शोषितों की एकता) उभर रहा है। यह एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसे जातीय विचारधारा के अधिकाधिक पंपिंग के द्वारा भी रोका नहीं जा सकता है।
साथियोंऔरदोस्तों!
पाषाण युग से लेकर आज तक का पूरा सफर एक बात सिखाता है: जाति इतिहास में पैदा हुई और आज पूंजीवाद (साम्राज्यवाद जिसकी सर्वोच्च अवस्था है) ने इसे जिंदा रखा हुआ है। खलिहानों व गोदामों पर अभी भी ताला लगा है, लेकिन उस ताले में जंग लग चुका है। जिन वर्गों ने तीन हजार साल तक वर्ण/जाति का मुखौटा पहना हुआ था, उनके मुखौटे अब उतर चुके हैं। असली उत्पादक आज के आधुनिक क्रांतिकारी सर्वहारा के तौर पर उनके सामने हैं – चाहे इतिहास ने उन्हें पहले कोई भी नाम दिया हो, चाहे उनकी जाति, धर्म या कम्युनिटी कुछ भी हो, आज वे सर्वहारा ही हैं, जिनका पूंजीपति वर्ग के हर हिस्से से कभी शांत या खत्म नहीं हो सकने वाला विरोध है।
इसलिए जाति विनाश का अगला और आखिरी कदम सर्वहारा को ही उठाना है, ठीक वैसे ही जैसे वर्गों को खत्म करना उनका काम है। जिस दिन वे खुद को उनके असली नाम – सर्वहारा – से बुलाएंगे, जिस दिन वे खैरात के टुकड़ों से इंकार कर पूरी रोटी और इसके स्रोत पर कब्जा मांगेंगे, वह दिन शासक वर्ग और उनकी जाति व्यवस्था का आखिरी दिन होगा। सुधार और आरक्षण (अफर्मेटिव एक्शन के तौर पर) ठीक हैं, लेकिन वे कुछ ही लोगों को संपन्न बनाते हैं जबकि करोड़ों को विपन्न बनाये रखते हैं। इसलिए हमें आंशिक सकारात्मक कदम मात्र नहीं, पूर्ण सकारात्मक कदम की जरूरत है। सवाल महज उत्पादित मालों और सेवाओं के वितरण में आंशिक दावेदारी की बात नहीं, बल्कि समस्त मेहनतकशों के पक्ष में उत्पादन के समस्त साधनों व स्रोतों के पुनर्वितरण और इस पर नये समाज के गठन का सवाल आज का प्रमुख सवाल है। जब सर्वहारा, अपने सभी अन्य मेहनतकश सहयोगियों व तबकों के साथ एकजुट होकर, सत्ता के शीर्ष की ओर बढ़ेगा, तो जाति और वर्ग दोनों एक ही आग में जलकर विनष्ट हो जाएंगे। तब एक नई इंसानियत पैदा होगी। एक नया इंसान पैदा लेगा।
शुरुआती इंसानों के पास सभ्यता का वह रास्ता अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं था जिसने ‘हड़पने वाले’ और ‘हड़पे गए’, कबीले, वर्ग, एस्टेट, राष्ट्रीयता, जातियां, वगैरह पैदा किए। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में हुआ। फिर भी, सर्वहारा वर्ग श्रृंखला में आखिरी कड़ी है – सभ्यता का आखिरी उत्पाद, ठीक वैसे ही जैसे पूंजीपति वर्ग आखिरी उत्पाद है। आने वाले समय में इंसान की कोई और अधीनस्थ किस्म नहीं आने वाली है। इसी तरह आज के पतनशील और विनाशकारी पूंजीपति वर्ग के बाद और कोई दूसरा वर्बर वर्ग पैदा नहीं लेगा। अगर इतिहास आगे बढ़ता है, तो अगले समाज का मालिक सर्वहारा होगा। अगर फासीवाद के तहत पहिया पीछे धकेला जाता है, तो हम बर्बरता और हिंदू राष्ट्र के पर्दे में छिपे मोनोपॉली वित्तीय पूंजी के नंगे वर्ग राज्य में पहुंच जाएंगे – उसके नियंत्रणाधीन और आज से कहीं अधिक मजबूत एवं कष्टकारी जाति व्यवस्था के अधीन।
जातियों की दुनिया के आगे वर्ग की दुनिया है, और इसकी आखिरी कड़ी सर्वहारा है। इसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे ही यह पहेली सुलझती है कि जाति की इस अंतिम बाधा को कौन तोड़ेगा।
सर्वहारा का जातियों और पहचानों में बंटवारा एक सांगठनिक मुश्किल है जिसे वर्ग-विरोधी और जाति-विरोधी संघर्ष को एक ही धारा में मिलाकर ही हल किया जा सकता है। वर्ग विरोधी संघर्ष अपने स्वभाव से ही जाति विरोधी है; अगर ऐसा नहीं है, तो यह फरेब है। जाति विरोधी संघर्ष जो साथ ही वर्ग विरोधी नहीं है, वह भी फरेब है। यह अकारण नहीं है कि आज के तथाकथित जाति नेता (जातिवादी नेता), जो सामाजिक न्याय के योद्धा होने का दावा करते हैं, जाति उन्मूलन या विनाश के बारे में एक शब्द भी नहीं उचारते।
सिर्फ सर्वहारा ही वर्गों की उस श्रृंखला को तोड़ सकता है और तोड़ेगा जिससे जातियां बनीं, और उसे कचरे की तरह फेंक देगा – सभी वर्गों और इंसानी किरदार पर उनकी छाप को मिटा देगा। यह एक ऐसा अध्याय शुरू करेगा जिसमें कोई शोषण, गुलामी, भेदभाव या गैर-बराबरी नहीं होगी। हालांकि यह पूरी तरह से नया अध्याय नहीं होगा: उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और शुरुआती नवपाषाण काल तक के इंसान भी सामाजिक रूप से वर्गविहीन और जातिविहीन ही थे। इंसान को वहां फिर से पहुंचना है। लेकिन कैसे? सत्तासीन सर्वहारा सारी सामाजिक दौलत – जमीन और उत्पादन के दूसरे सभी साधन – हासिल करके उन्हें सामाजिक मालिकाना हक में लाएगा, तकनीक में महारत हासिल करेगा और अभावग्रस्ता से दूर सामाजिक उत्पादन की प्रचुरता का समाज बनाएगा और इस तरह बिना पाषाण युग में वापस जाए ही इंसानियत को फिर से वर्गविहीन और जातिविहीन बना देगा। विजयी सर्वहारा वर्ग आदेश देगा – सब सबके लिए, यानी एक दूसरे के लिए काम करेंगे। इस तरह निजी हित सामूहिक हित, जो पूंजीवादी संबंधों की वजह से एक-दूसरे के खिलाफ प्रतीत होते हैं, के साथ एकाकार हो जाएंगे। निजी संपत्ति सिर्फ निजी इस्तेमाल तक सीमित होगी। जड़ीभूत श्रम विभाजन का अंत हो जाएगा; शहर-गांव का फर्क भी इसी के साथ मिट जाएगा।
इस तरह, जाति का खत्म होना आखिरकार इस बात पर निर्भर करता है कि मजदूर वर्ग सत्ता पर कब्जा करता है और वर्ग खत्म करता है या नहीं। बीसवीं सदी के पहले आधे हिस्से की मजदूर वर्ग की क्रांतियों, खासकर सोवियत संघ में मजदूर वर्ग के शासन के अनुभव ने साबित कर दिया कि यह मुमकिन है। जिस पल मजदूर वर्ग शासक वर्ग बन जाता है, वह ऐतिहासिक रूप से वर्ग नहीं रह जाता – इंसानियत के आम हित के अलावा उसका कोई खास हित नहीं रह जाता। सत्ता में मजदूर वर्ग यह ऐलान करके भी इसे जाहिर करेगा: जो काम नहीं करेगा, वह खाएगा नहीं; मजदूरी की गुलामी पर पाबंदी; पैदावार की चीजें सबकी हैं; इस्तेमाल पहले मेहनत के हिसाब से होगा, बाद में जरूरत के हिसाब से। कुदरत के अंधे नियम काम करना बंद कर देते हैं; मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि इंसानी आजादी के लिए बना समाज एक हकीकत बन जाता है।
इसलिए, मजदूर वर्ग का सत्ता में आना एक ऐसे क्रांतिकारी इंसान का इतिहास के ड्राइविंग सीट पर आ बैठना है जो ‘हड़पने वाले’ और ‘हड़पे गए’ के दौर को पूरे तरीके से खत्म कर देगा। यह एक ऐसे इंसान का आगमण होगा जिस पर न तो वर्ग की छाप होगी और न ही जाति की। सिर्फ ऐसे ही भौतिक परिवेश में जातियां पूरी तरह खत्म हो सकती हैं, समाजवाद से कम्युनिज्म में बदलाव के दौर की पीढ़ियों की यादों से पूरी तरह से गायब हो सकती हैं।
यह याद रखना चाहिए कि जाति और वर्ग दोनों ही अतीत की निरंतरता हैं, लेकिन वर्ग अधिक लंबी और ज्यादा बुनियादी निरंतरता है। बदलते वर्ग संबंधों के साथ जाति को बार-बार पुनर्संगठित होना पड़ा है; यह सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि वर्ग बना हुआ है। वर्ग को खत्म करने से जाति का भी वही हश्र होगा।
यह भी सच है कि वर्ग एकता के अंदर भी जाति-विरोधी और जातीय मानसिकता-विरोधी संघर्ष की जरूरत है ताकि वर्ग-संघर्ष जाति के भेदभाव और जाति की मानसिकता से दूषित न हो। इसे असली वर्ग एकता की अग्नि परीक्षा होना चाहिए। असली चुनौती – और इस कन्वेंशन का असली उद्देश्य व काम – आंदोलन के अंदर और बाहर, सिद्धांत रूप में और रोजाना व्यवहार में, जाति-विरोधी और वर्ग-विरोधी संघर्ष का परस्पर संलयन कैसे हो, यही है। हम अपने प्रिय क्रांतिकारी प्रतिभागियों से कहना चाहते हैं: आइए हम सब मिलकर कन्वेंशन को इस लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक ले जाएं।
आखिर में, हम कन्वेंशन द्वारा मंजूरी के लिए ये प्रस्ताव (जिनकी पूरी जानकारी अंत की टिप्पणियों में दी गई है) रखते हैं। इन पर सुझावों का पुरजोशी से स्वागत है, साथ ही प्रस्तावों को पारित करने का अनुरोध भी है।
- ‘प्रतिरोध के अधिकार’ की मांग उठायें और जातिगत जुल्म एवं छुआछूत के खिलाफ बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएं।1
- जाति विरोधी वैचारिक अभियान खड़ा करने हेतु –
- सामाजिक श्रम में भागीदारी के हिसाब से जमीन समेत समस्त सामाजिक दौलत के पुनः बंटवारे की मांग उठाकर जाति-विरोधी सोच वाला आंदोलन खड़ा करें;
- “जो काम नहीं करेगा, वह खाएगा नहीं” का झंडा उठाएं;
- एक ऐसे मजदूर राज्य का झंडा उठाएं जो ऊपर बताई गई मांगों को पूरा करेगा और मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व लागू कर उनकी पूर्ति में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करेगा;
- हर साल एक तय तारीख को देश भर में रैलियां, आदि आयोजित कर जाति विनाश की विचारधारा का झंडा लगातार उठाएं;
- सर्वहारा नजरिया आधारित जाति-विरोधी संगठन बनाएं;
- जाति और वर्ग दोनों को खत्म करने के लिए अभियान चलाएं;
- जनता की जाति-विरोधी चेतना बढ़ाने हेतु सभी राज्य-स्तरीय और आम चुनावों में जाति उन्मूलन का झंडा और विचार बुलंद करें।2
- समाजवादी भूमि सुधारों के लिए लड़ें। इससे जमीन प्राइवेट मालिकाने से आजाद होगी। सर्वहारा राज्य में, जमीन पर वे लोग मिलकर खेती करेंगे जो अपनी मेहनत से काम करते हैं। इससे ही गांवों में जाति के जुल्म की बुनियाद खत्म होगी।
- अंतर्जाति शादियों को बढ़ावा दें, उनका जश्न मनाएं और मौजूदा धार्मिक पर्सनल तथा सिविल विवाह कानूनों में आयद पाबंदियों के खिलाफ सभी को अपनी पसंद के साथी से विवाह के अबाध अधिकार के लिए आवाज उठाएं। हालांकि सिर्फ इससे जाति खत्म नहीं होगी, लेकिन इससे अंतर्विवाह के नियम को तोड़ने में मदद मिलेगी, जो आज भी जाति व पितृसत्ता की अभिन्न साझा सोच का मुख्य आधार है।
- आवासीय व्यवस्था, विशेषकर भाड़े के आवासों में जाति-सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव को रोकने हेतु समस्त शहरी जमीनों के समाजीकरण और सभी के लिए सामाजिक आवासीय व्यवस्था के लिए संघर्ष करें। ग्रामीण आवासीय भूमि के समान वितरण द्वारा सभी के लिए आवासों की गारंटी की मांग उठाएं।
- उत्पीड़ित जातियों की जनता को हाशिए पर डालने वाली अति गैरबराबरी को मिटाने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मनोरंजन, आदि क्षेत्रों में समान सार्वत्रिक सार्वजनिक अधिकार की गारंटी के लिए संघर्ष करें।
- सभी सामाजिक संघर्षों की मुख्य कड़ी के तौर पर क्रांतिकारी अभियानों को तेज करें।3
टिप्पणियां:
- कुछ बुर्जुआ कानून हैं जो जाति के आधार पर होने वाले जुल्म और छुआछूत का निषेध करते हैं। जब हम देखते हैं कि ये कानून असल में कैसे काम करते हैं, तो उनकी असली वर्ग प्रकृति सामने आती है। उदाहरण के लिए, SC/ST (अत्याचार रोकथाम) एक्ट और दूसरे छुआछूत विरोधी कानून दबे हुए लोगों को एक ऐसी सरकारी मशीनरी के रहमोकरम पर छोड़ देते हैं जो जुल्म करने वाले के पक्ष में बहुत ज्यादा भारी है। इसके अलावा, ये कानून दबे हुए लोगों को लंबी अदालती लड़ाइयों में घसीटते हैं जहाँ वे एक बार फिर पैसे और ताकत के रहमोकरम पर होते हैं। आखिर में, मौजूदा कानून किसी भी तरह से दबे हुए लोगों को बाहर आने, विरोध करने और जुल्म करने वाले का विरोध करने के लिए बढ़ावा नहीं देते हैं। इसके उलट, अगर दबे हुए लोग विरोध करने की हिम्मत करते हैं, तो उन्हें भी उतना ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और “कानून अपने हाथ में लेने” के नाम पर सजा दी जाती है।
इस तरह, इन कानूनों का वर्ग चरित्र पूरी तरह से सामने आ जाता है।
ठीक इसलिए क्योंकि बुर्जुआ कानून के तहत सीधा विरोध करना सजा है, हमें विरोध करने के अधिकार की मांग उठानी चाहिए और उसके लिए लड़ना चाहिए। इसमें पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध के आह्वान को कानूनी काम बनाने की मांग भी शामिल है। जाति के जुल्म और छुआछूत के खिलाफ हमारी लड़ाई का यही मुख्य मुद्दा है।
- इतिहास में हमारे सामने दलित पैंथर्स आंदोलन रहा है, जो मुख्य रूप से दो बुनियादी सवालों से जुड़ा था: जाति का खात्मा और हर तरह के जुल्म और छुआछूत का विरोध करने का अधिकार। दलित पैंथर्स के लिए, “दलित” में काम करने वाले लोग और महिलाएं शामिल थीं, इसके अलावा पहले के अछूत (SC और ST समुदायों के लोग) भी शामिल थे। “दलित” शब्द का मतलब सिर्फ पीड़ित होना नहीं था, बल्कि एक सक्रिय, मजबूत ताकत थी जो जाति के जुल्म, जातिगत असमानता और खुद जाति की सोच का विरोध करती थी।
खासकर, जाति व्यवस्था और जाति की सोच के खिलाफ इसकी प्रबल प्रेरणा आज भी हमारी कल्पना को छूती है। उस समय के मशहूर दलित विचारक, प्रोफेसर गंगाधर पंतवने ने कहा था: “दलित कोई जाति नहीं है। वह इस देश की सामाजिक और आर्थिक परंपराओं द्वारा शोषित एक आदमी है।” इस तरह, जाति की सोच से लड़ना आज के समय के सबसे बुनियादी तरक्कीपसंद और क्रांतिकारी कामों में से एक है। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जाति के खात्मे का झंडा सबसे पक्के इरादे से उठाया जाए, जिसमें हर जाति और समुदाय में नए वर्ग रिश्तों और पूंजीवादी तबके के उभरने को पूरी तरह ध्यान में रखा जाए। यह कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसा कि प्रस्ताव 2 में बताया गया है।
- आज हम जो देख रहे हैं, वह यह है: दो प्रक्रियाएं एक साथ और एक-दूसरे के समांतर जारी हैं।
एक तरफ, मोनोपॉली पूंजी की बहुत ज्यादा लूट से बनी भौतिक स्थिति सभी समुदाय के शोषित लोगों में एकता की चाहत जगा रही है, जो जाति (चाहे सवर्ण हो या अवर्ण) और यहां तक कि धर्म, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, की सीमाओं को पार कर रही है। यह एकता भयंकर शोषण के असर में अपने आप उभर रही है। गरीबों में बहुत ज्यादा निराशा की भावना फैली हुई है, जिससे एक ही जाति (सवर्ण या अवर्ण दोनों) के अंदर एक नए तरह का विकर्षण और फूट पैदा हो रही है और साथ में, सभी जातियों में एक नए तरह का वर्ग आधारित विलय और एकता पैदा हो रही है। जाति की सोच के बड़े पैमाने पर फैलने के बावजूद यह बहुत तेजी से हो रहा है। हम पहले से ही कड़े विरोध के बावजूद अंतर्जाति और अंतर-सामुदायिक शादियों में बढ़ोतरी देख रहे हैं। सभी के लिए नौकरियों की लड़ाई ही दबे-कुचले लोगों के लिए नौकरियों की एकमात्र असली गारंटी बन गई है। बड़ी पूंजी की कभी न खत्म होने वाली मुनाफे की चाहत से होने वाले निजीकरण से सिर्फ एक होकर ही लड़ा जा सकता है। सबके लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की लड़ाई ही दबे-कुचले समुदायों के लिए एक अच्छे भविष्य की एकमात्र गारंटी बन गई है, क्योंकि मोनोपॉली पूंजी तेजी से इन सेक्टरों को ऐसे क्षेत्रों में बदल रहा है जहाँ हर जाति के गरीब पहुँच ही नहीं सकते। संक्षेप में, आज का अत्यधिक वर्गीय शोषण और लूट सभी गरीबों में वर्ग चेतना बढ़ा रहा है, भले ही सत्ताधारी पूंजीपति इस अपने आप होने वाली वर्ग एकता की प्रक्रिया में रुकावट डालने और उसे धुंधला करने के लिए जाति और सांप्रदायिक सोच फैलाने पर तुले हुए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूंजीपति तबके की (बड़ी पूंजी के साथ मिलीभगत में) जाति की सोच फैलाने की कोशिश में अपने आप कमी आई है; इसे लगातार बढ़ावा देना और सहारा देना पड़ता है। इसके उलट, दबे-कुचले और शोषित लोगों में वर्ग एकता की भावना सभी मुश्किलों और विरोधी वजहों के बावजूद अपने आप और स्वाभाविक रूप से बन रही है। इस तरह, शोषण, असमानता और भेदभाव का सामना करने वाले सभी लोगों की वर्गीय एकता एक ऐतिहासिक जरूरत बन गई है। समय की जरूरत साफ है: हमें वर्ग विरोधी और जाति विरोधी चेतना को मिलाना होगा और उसी के हिसाब से व्यवहारिक कार्यक्रम बनाने होंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ स्वतःस्फूर्तता अपर्याप्त है। स्वतःस्फूर्तता को मंजिल पर पहुंचाने के लिए सचेत दखल की जरूरत होती है, ताकि जो चीजें असल और ऐतिहासिक रूप से जरूरी हैं, उन्हें सबसे आगे लाया जा सके और वे एक अकेली, संगठित ताकत के तौर पर पूरी घटनाओं को नेतृत्व दे सकें। जिस पल हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएँगे, जीत हमारी होगी।
_________________
पुनश्च:
- इसके अतिरिक्त 6 अक्टूबर 2024 को पहले जाति विरोधी कन्वेंशन में पेश किया गया हमारा आधारपत्र भी https://yatharthmag.com/caste-annihilation-6oct24/ पर पढ़ा जा सकता है।
- कुछ बिंदुओं की व्याख्या हेतु विस्तृत ऐतिहासिक टिप्पणियां हैं, जिन्हें इस प्रपत्र को छोटा रखने के लिए यहां शामिल नहीं किया गया है। जो साथी चाहें, उनके द्वारा मांगने पर, उन्हें भेजा जा सकता है।
क्रांतिकारी अभिवादन सहित
Proletarian Peoples Front / सर्वहाराजनमोर्चा